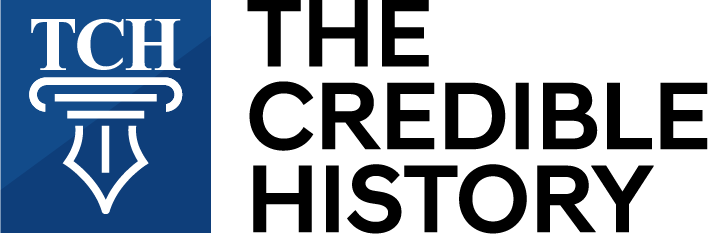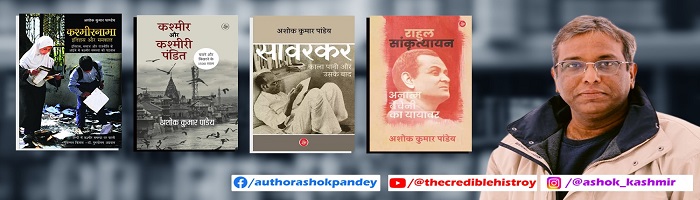[जाने-माने हेरिटेज एक्टिविस्ट सोहेल हाशमी दिल्ली के शहर बनने की कहानी के साथ बात रहे हैं कि आखिर ‘शहर कैसे बनते हैं?’।
पढ़िए इसकी तीसरी क़िस्त। ]
शहर क्या है III
इस बात का ज़िक्र तो पहले हो ही चुका है कि तीन चीज़ें किसी आबादी को शहर बनाने के लिए दरकार हैं- प्रवासी, लेन-देन और समय। इनमें से प्रवासियों के बारे में हम पिछले सप्ताह बात कर चुके हैं, इस बार लेन-देन के बारे में बात करते हैं।
जिस लेन-देन की बात हम कर रहे हैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा व्यापार है। उससे कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा उस लेन-देन, अदला-बदली या तबादले का है जिसमें पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाता मगर वो सब कुछ आता-जाता है जो असल में मायनों में ज़िन्दगी को बेहतर बनाता है और यह लेन-देन होता है बाहर से आने वालों और उस बस्ती में रहने वालों के दरम्यान।
बाहर से आने वाले लोग, नए औज़ार, नए मसाले, नए बर्तन, खाना पकाने के नए तरीक़े, नए पकवान, नए कपड़े, संगीत के नए यंत्र, नई भाषाएँ, निर्माण के नए तरीक़े और दूसरी बहुत सी चीज़ों के साथ एक नया सौन्दर्य बोध ले कर आते हैं। यह सब कुछ जो प्रवासियों के साथ आता है वो अपने स्थानीय समकक्षों के साथ मिलता है और इस मेल-मिलाप से कुछ नया पैदा होता है।
ठीक वैसे ही जैसे 1947 से पहले की दिल्ली, जिस की ज़बान मुख्यतः उर्दू थी, साल भर के अंदर-अंदर पंजाबी, मुल्तानी, सिन्धी आदि भाषाओं और उन ज़बानों के बोलने वालों की जीवन शैली के असर में तब्दील होने लगी। अचानक ही शहर की आबादी ही बदल गयी, उर्दू बोलने वाले चले गए और दिल्ली पंजाबी बहुल इलाक़ा हो गया।
अब पिछले 50 वर्षों में धीरे-धीरे पूर्वांचल से भोजपुरी बोलने वालों के आने से, दिल्ली वालों की भाषा, भोजन और लिबास में धीरे-धीरे एक और बदलाव आने लगा है। लिट्टी-चोखा अब मेट्रो स्टेशन्स के बाहर और दिल्ली के अलग-अलग इलाक़ों में मिलने लगा है और कांधे पर गमछा डाल कर चलना फैशन का हिस्सा बनने लगा है।
शहर ऐसे ही बदलते रहते हैं, कभी धीरे-धीरे कभी तेज़ी से। हमेशा कुछ पुराना बचा रहता है और कुछ नया उसमें मिल जाता है। जहाँ ऐसे बदलाव नहीं आते, वहाँ के जीवन में एक ठहराव सा रहता है, जैसा गाँव के जीवन में होता है। परिवर्तन की नई हवाएं, प्रवासी ले कर आते हैं, वो स्थानीय, मूल निवासियों की ज़िन्दगी में अपने आप पैदा नहीं होती।
इस खुले स्वछन्द लेन-देन के लिए ज़रूरी है, आपसी मेल-मिलाप। जब तक किसी आबादी के मूल निवासियों और बाहर से आने वाले प्रवासियों के बीच मिलना -जुलना नहीं होता यह लेन-देन मुमकिन ही नहीं है।
आज-कल दिल्ली में बनने वाली ‘कॉलनीज़’ जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों और लोहे के फाटकों से घिरी हैं, उनमें यह सांस्कृतिक लेन-देन संभव ही नहीं है।
जब तक एक ही जैसी सोच रखने वाले लोग, अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ ही रहते रहेंगे तब तक परिवर्तन की नई हवाओं के बहने के लिए कोई रास्ता बन ही नहीं सकता। हम ख़ुशकिस्मत हैं कि ऐसी बस्तियां जिनमें बाहर की हवा आने के लिए कोई रास्ता ही ना हो, उस समय में नहीं थीं जब बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, इंदौर, मेरठ, भोपाल, लाहौर, जबलपुर, पटना, अमृतसर, लुधियाना, अहमदाबाद, हैदराबाद, मैसूर, कोचीन वगैरह जैसे शहरों का उदय हो रहा था। इनमें से हर शहर में अलग-अलग भाषा बोलने वाले, अलग-अलग तरह के कपड़े पहनने वाले, अलग-अलग तरह के मकान बनाने वाले, अलग-अलग तरह के काम करने वाले लोग आ कर बसते रहे और इस तरह यह पुरानी आबादियाँ शहरों में तब्दील हुई।
इसी विविधता ने हमारी सतरंगी संस्कृति को जन्म दिया, विकास की संभावनाएं पैदा की और हमारे एक ऐसे समाज का निर्माण करने की क्षमताएं प्रदान कीं जो अपने तमाम अंतर-विरोधों के बावजूद, या शायद उन्हीं की वजह से, संसार में सबसे अधिक विविधता पूर्ण सह-अस्तित्व की अनोखी मिसाल कायम हो पाई।
इन तीन छोटे लेखों पर आधारित इस पृष्ठभूमि को हम आगे आने वाली कड़ियों में दिल्ली पर लागू करके देखेंगे, ताकि यह समझने में मदद मिले कि दिल्ली, दिल्ली कैसे बनी।
—
इस शृंखला के अन्य लेख
1- पहली कड़ी
2- दूसरी कड़ी
क्रेडिबल हिस्ट्री का प्रोजेक्ट जनसहयोग से ही चल सकता है। जनता का इतिहास जनता ही लिखेगी और जनता को ही इसकी जिम्मेदारियाँ उठानी होंगी।
बड़ी-बड़ी फन्डिंग वाले प्रॉपगेंडा से टकराने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए।
हेडर पर subscription Link है, यहाँ क्लिक करें और यथासंभव सहयोग करें।
सबस्क्राइब करने पर आपको मिलेंगी हमारे तरफ़ से कुछ विशेष सुविधाएं.

जाने-माने हेरिटेज एक्टिविस्ट, दिल्ली के इतिहास पर विशेष काम।