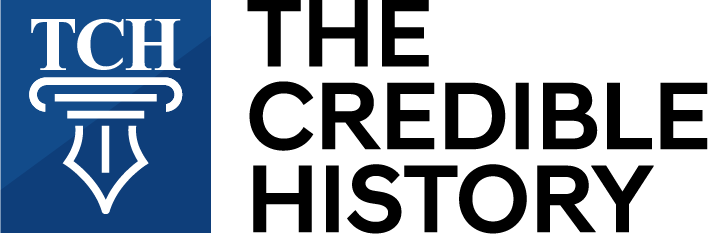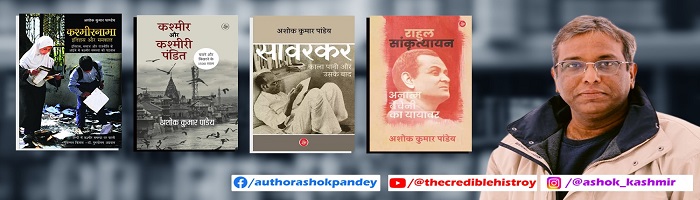मई दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। श्रम यानी सिर्फ़ मर्दों का श्रम? औरतों की मेहनत पर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्यों अलक्षित रह जाता है घर से बाहर तक का स्त्री-श्रम? पढ़िए यह विशेष आलेख – सं
घर का काम तुम्हारा और बाहर का हमारा
पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में माँ के किरदार को याद करते हुए अक्सर एक चेहरा निरूपा राय जैसी माँ का सामने आता है, जो विधवा है, दुखी है, लेकिन स्वाभिमानी है। पति के न रहने पर वह दिन-रात दूसरों के कपड़े सिल कर अपने बच्चों को बड़ा करती है.
अचानक यह एहसास होता है कि दुनिया का सारा कारोबार पुरुष के श्रम पर चलता है और स्त्री इसमें केवल मर्द के न रहने पर ही मजबूरी में आती है. उसका सारा श्रम घरेलू श्रम है, जिसका कोई मूल्य नहीं है और इस तरह मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से घरेलू औरत का श्रम गिनती से बाहर का हो जाता है।
‘घर का काम तुम्हारा और बाहर का हमारा’ वाले श्रम के लैंगिक विभाजन का एक बड़ा प्रचलित हिस्सा एक फरेब है, क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े जुटाते हैं, तो बड़ी संख्या में घर पर काम करके कमानेवाली औरतों की बड़ी संख्या अदृश्य होती है।
ऐसे श्रम जिसका किसी गणना में आना असंभव
वह संख्या न सिर्फ़ घर के काम करती है, बल्कि अचार-पापड़ बना कर, ऊनी कपड़े बुन कर, कढ़ाई वगैरह करके पति की कमाई में अपना हिस्सा जोड़ती है, ताकि घर को ठीक से चला सके, बच्चों को कुछ और सुविधाएं मिल सकें। बीड़ी, अगरबत्ती, टोकरियाँ, कारपेट आदि बनाने के लघु उद्योग औरतों के श्रम से चलते हैं. यह गैर-संस्थागत तरीक़े से हो, तो ऐसे श्रम का कहीं किसी गणना में आना असंभव है.
ऐसे जाने कितने ही काम हैं, जहाँ पुरुष श्रम करता नज़र आता है, लेकिन उसके घंधे के लिए तैयारी करनेवाली स्त्री पर्दे के पीछे छिप जाती है। खेतों में श्रम करना, गाय-बैल की पानी-सानी करना और बाकी बेहुनर (Unskilled) काम स्त्रियाँ करती आयी हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में 83 प्रतिशत औरतें हैं, जबकि जिन ज़मीनों पर उनका श्रम लगता है, उनका मालिकाना हक़ पुरुषों के पास है। पहाड़ों पर अक्सर औरतें घर देखने के साथ-साथ खेती, बुनाई जैसे काम करती हैं।
लकड़ियाँ ढोते या पीठ पर गैस सिलेंडर ढोते दिखती हैं, तो पता चलता है कि इस ‘घर देखने’ में पहाड़ जैसे मुश्किल भूगोल में पहाड़ जैसा श्रम उन्हीं का है।
छोटे दुकानदारों के घर की स्त्रियाँ उनके लिए सूखे मेवे वगैरह के पैकेट बनाती हैं. ठेला लगा के छोले-भटूरे आदि बेचनेवाले पुरुषों की स्त्रियाँ व्यंजनों को बनाने में मदद करती हैं।
इसके अलावा भी, बाज़ार उनका श्रम बेहद सस्ते दामों में खरीदता है। किसी मैचिंग सेंटर पर से साड़ियाँ घरों तक भेजी जाती हैं और घर के काम से फुरसत पाकर कुछ औरतें उन पर फॉल लगाती हैं, लहंगे और चुन्नियों पर सलमे-सितारे लगाती हैं. देसी बीड़ी बनाने के उद्योग में बड़ी संख्या में औरतें हैं।
चाय के बागानों में काम करनेवाली औरतें हैं. यह ऐसा श्रम है, जो बिजनेस के आंकड़े इकट्ठे करते हुए अनदेखा चला जाता है. बिजनेस या दुकानें भी स्त्रियों की नहीं होतीं। भवन-निर्माण के कामों में लगी उन मज़दूर औरतों का श्रम भी हमें नज़र नहीं आता, जो निर्माण-स्थल पर खाना बनाने के वक़्त खाना बनाती हैं और बाकी वक्त अपने मज़दूर पति की हेल्पर बन जाती हैं।
ऐसे बेहुनर, अप्रशिक्षित श्रम की कोई वाजिब क़ीमत बाज़ार के पास नहीं है, इसके लिए कोई आंकड़े नहीं हैं, इस श्रम की कहीं कोई पहचान और इसका सम्मान नहीं है।
https://thecrediblehistory.com/leaders/others/international/history-of-may-day/
भारतीय परिवार संरचना अलक्षित स्त्री-श्रम
भारतीय परिवार संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि बाज़ार ने स्त्री श्रम का बहुत शातिर तरीक़े से इस्तेमाल किया है. स्त्रियाँ घर के बाहर नहीं जा सकतीं काम करने के लिए। सुबह से शाम तक जब घर के मर्द बाहर रहते हैं, उनके पास एक बड़ा खाली वक़्त है, जिसका आकलन किया गया।
साथ ही औरतों को अपने पे-रोल पर सीधे रखने में नियोक्ताओं को जो पचड़े हो सकते हैं- मातृत्व अवकाश, बच्चा पालन अवकाश, बीमारी-तीमारदारी वगैरह- उन सबसे भी मुक्ति हो जाती है। एक गर्भवती कर्मचारी सीधे-सीधे बिजनेस के लिए एक घाटा है।
घरेलू औरतों की यह ज़रूरत का, कि खाली वक़्त में बैठे-बैठे (?) चार पैसे कमाये जा सकें, फायदा औरत को कितना हुआ, यह एक शोध का मुद्दा है। क्योंकि, इस तरह हाथ में आये चार पैसे भी उसी पितृसत्तात्मक परिवार संरचना को बनाये रखने में खप जाते हैं, जिसे स्त्री की आर्थिक या किसी भी तरह की आत्मनिर्भरता से दिक़्क़त होती है।
यह सस्ता श्रम है। स्त्रियाँ काम के हिसाब से बेहद कम पैसा पाती हैं। बीड़ी खरीद में जब ग्राहक सौ रुपये देता है, उसमें से सिर्फ ग्यारह रुपये ही इन स्त्रियों तक पहुंचता है। ग्रामीण श्रेत्रों में अगरबत्ती निर्माता तो ज्यादातर औरतों को ही इस काम के लिए रखते हैं।
औरत बाजार की एजेंट हुई, फ़ायदा हुआ बाज़ार को
शहरों में बाजार ने मध्यवर्गीय उपभोक्ता स्त्री और उत्पाद की मार्केटिंग करनेवाली स्त्री को आमने-सामने कर दिया है। खर्चीले विज्ञापनों से बचते हुए टपरवेयर, ओरीफ्लेम और एमवे जैसे उत्पादों ने शहरी घरेलू औरत के खाली वक़्त और पैसे की ज़रूरत को एक साथ । पुरुष सेल्समैन से अधिक विश्वसनीय यह पड़ोसन-सी औरत बाजार की एजेंट हुई, तो उसे भी फ़ायदा हुआ और बाज़ार को भी।
पितृसत्ता को इससे कोई खतरा भी नहीं हुआ कि औरत को बाहर नौकरी करने नहीं जाना पड़ा। यह सुरक्षित भी था कि उसे औरतों से ही डील करना था।
यही नहीं, पिछले बीस-पच्चीस सालों में जिस तरह गली-नुक्कड़ में प्ले स्कूल और पब्लिक स्कूल मशरूम की तरह उगने शुरू हुए, उनके लिए घरेलू महिलाएं, प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित, सस्ता श्रम साबित हुईं, जिन्होंने काम करने की शर्तों और पारिश्रमिक से समझौता किया। यह भी पितृसत्ता के लिए फ़ायदे का ही सौदा हुआ कि शादी के बाज़ार में भी टीचर-बहू की मांग बढ़ गयी, जो घर के काम निबटाने के साथ-साथ चार पैसे कमा रही थी।

सुजाता दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। कवि, उपन्यासकार और आलोचक। ‘आलोचना का स्त्री पक्ष’ के लिए देवीशंकर अवस्थी सम्मान। हाल ही में लिखी पंडिता रमाबाई की जीवनी, ‘विकल विद्रोहिणी पंडिता रमाबाई’ खूब चर्चा में है।