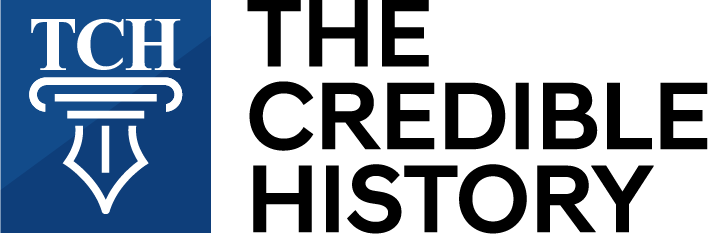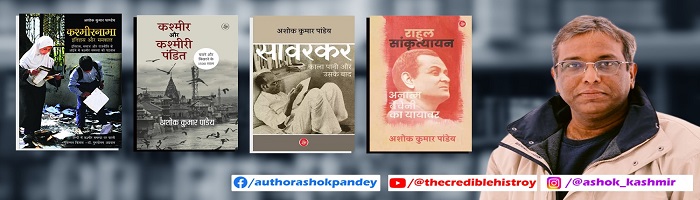जाति, पूना पैक्ट और गांधी

[गांधी और जाति के सवाल पर बहुत कुछ कहा जाता है। आज उस पर ही कुछ बात।]
बारडोली से चंपारण तक गांधी देख पा रहे थे कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन अन्याय से भरा हुआ है। दमन और शोषण इसके हथियार हैं। इस भाषण में जो बीज थे वे बाद की घटनाओं में फलते-फूलते दिखते हैं और कराची अधिवेशन तक स्वराज की अवधारणा में अंग्रेज़ों की विदाई की बात पूरी ताक़त से शामिल होती है। नमक सत्याग्रह और जालियाँवाला बाग़ कांड ऐसी दो घटनाएँ थीं जिन्होंने गांधी के इस विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई कि ब्रिटिश राज्य न्यायपूर्ण राज्य है। गोरों की श्रेष्ठता का सिद्धान्त अब उनके सामने नंगा था जिसमें भयावह नस्ली अहंकार और दूसरों के प्रति घृणा भरी हुई थी। शायद इसी अनुभव ने उन्हें अफ़्रीका और योरप के अश्वेतों के बारे में नए सिरे से सोचने का मौक़ा दिया। अफ्रीका प्रवास के दौरान अश्वेतों के दमन पर चुप रहने वाले गांधी अपने जीवन के आख़िरी दौर में कई बार उनके पक्ष में आवाज़ उठाते दीखते हैं। उदाहरण के लिए जब ब्लैक अमेरिकियों के एक समूह ने अगस्त 1924 में इन्हें एक तार भेजा, तो उसका जवाब उन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में देते हुए लिखा :
उनका काम हमारी तुलना में बहुत कठिन है, लेकिन उनके बीच कुछ बहुत ही अच्छे काम करने वाले लोग है। इतिहास के कई छात्र मानते हैं कि भविष्य उनके साथ होगा, उनकी काया अच्छी है, उनके पास गौरवशाली कल्पना है, वे उतने ही सरल हैं जितने वे बहादुर है। फिनोट ने अपने वैज्ञानिक शोधों से ये साबित किया है कि उनमें कोई अंतर्निहित हीनता नहीं है , उन्हें बस अवसर की आवश्यकता है।[ii]
इसी तरह 30 जून 1946 को साप्ताहिक पत्र हरिजन में गांधी लिखते हैं –
गोरे लोगों की वास्तविक जिम्मेदारी काले या अश्वेत लोगों पर अक्खड़पन से हावी होना नहीं है, यह उस पाखण्ड से दूर होना है जो उन्हें खाए जा रहा है। यह वह समय है जब गोरे लोगों को सभी से समान व्यवहार करना सीखना चाहिए। श्वेत त्वचा अब कोई रहस्य नहीं है। अब यह बारम्बार सिद्ध हो चुका है कि अगर किसी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाये तो चाहे वह किसी भी रंग या देश का हो, वह किसी भी अन्य के पूरी तरह से बराबर है।[iii]
इसका सबसे मुखर स्वर 17 नवम्बर, 1947 को उनकी आख़िरी प्रार्थना सभाओं में से एक में दिए गए भाषण में मिलता है –
दक्षिण अफ्रीका में कई विद्वान पुरुष और महिलाएँ हैं…यह एक वैश्विक त्रासदी होगी अगर वे अपने दुर्बल परिवेश से ऊपर नहीं उठते और गोरों के वर्चस्व की इस दुखद और चिंताजनक समस्या को चुनौती नहीं देते। क्या अब यह खेल बहुत नहीं खेला जा चुका है?[iv]
ज़ाहिर है अपने आख़िरी समय तक वह गोरों के वर्चस्व के खेल को ख़त्म करने के पक्ष में थे और उसमें अपनी सक्रिय भूमिका भी निभा रहे थे।
गांधी के मूल प्रस्ताव जिनपर वह अडिग रहे
यहाँ एक और बात कहनी ज़रूरी होगी। भारत आने से पहले वह हिन्द स्वराज लिख चुके थे। इस ‘स्वराज’ में अंग्रेज़ों से मुक्ति की बात नहीं थी। यहाँ अंग्रेज़ी संस्कृति से या यो कहें पश्चिमी संस्कृति से मुक्ति की बात थी, वह अंग्रेज़ों को बाहर निकालकर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित भारत बनाने की जगह भारतीय मूल्यों पर आधारित जीवन शैली तथा प्रशासन की वकालत कर रहे थे। यह पश्चिमी तार्किकता और विज्ञान को एकदम परे रख भारतीय क़िस्म की आधुनिकता को विकसित करने की उनकी कोशिश थी जो टैगोर सहित अपने समकालीनों से बिलकुल अलग थी। छूआछूत दूर करना और हिन्दू-मुस्लिम एकता इसके सबसे आवश्यक सामाजिक मूल्य थे तो भारी उद्योगों पर संकेन्द्रण की जगह छोटे, श्रमसघन अर्थात मशीन की जगह मानव श्रम पर आधारित उद्योग इसके आर्थिक आधार थे और अहिंसा तथा सत्याग्रह इसे हासिल करने के तरीक़े। आप देखते हैं कि बाक़ी चीजें आती-जाती हैं लेकिन इन मूल प्रस्तावों पर गांधी कभी कोई समझौता नहीं करते। गोलमेज़ सम्मलेन के दौरान अमेरिकी रेडियो को दिए साक्षात्कार में वह कहते हैं –
मेरा दृढ़ मत है कि कोई भी व्यक्ति बिना अपनी कमज़ोरियों के आज़ादी को नहीं खोता। मैं कष्टपूर्वक अपने देश की कमज़ोरियों के प्रति चेतन हूँ। भारत में दुनिया के हर धर्म का प्रतिनिधित्व है और यह स्वीकार करना एक शर्मनाक हकीक़त है कि हम आपस में बंटे हुए हैं ; यह कि हम हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह मेरे लिए और गहरे शर्म की बात है कि हिन्दू अपने ही लाखों भाई-बन्दों को छूने से परहेज़ करते हैं। मैं कथित अछूतों की बात कर रहा हूँ।
आज़ादी के लिए लड़ रहे देश में ये कोई छोटी कमज़ोरियाँ नहीं हैं। आप देखेंगे कि आत्मशुद्धि के इस संघर्ष में हमारे लोगों का बड़ा हिस्सा लगा है। हम अस्पृश्यता के इस श्राप से मुक्ति और भारत में रहने वाले सभी तरह के लोगों के बीच एकता स्थापित करने में लगे हुए हैं।[v]
अफ्रीका से लौटने के बाद वह लगातार छूआछूत का विरोध कर रहे थे। यही नहीं, धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करने वाले गांधी मनुस्मृति को लेकर आलोचनात्मक थे। जब उनके छूआछूत विरोधी अभियान पर रूढ़िवादियों ने मनुस्मृति के सहारे हमला करने की कोशिश की तो गांधी ने नवंबर 1917 में गोधरा में अन्त्यज सम्मलेन में भारत के माथे पर एक दाग़ विषय पर बोलते हुए कहा –
हिन्दू धर्म, धर्म के नाम पर अनेक पापों से भर गया है। ऐसी रूढ़िवादिता को मैं पाखण्ड कहता हूँ। आपको ख़ुद को इस पाखण्ड से मुक्त करना होगा; जिसका फल आप ख़ुद भुगत रहे हैं। मनुस्मृति या ऐसे धर्मग्रंथों से इस रूढ़िवादिता के पक्ष में श्लोक संदर्भित करना बेकार की बात है। बहुतेरे श्लोक अप्रमाणिक हैं और उनमें से तमाम तो कतई बेमतलब हैं।[vi]
गांधी ने 1927 के महार सत्याग्रह का भी खुल समर्थन किया।
यह आंदोलन पश्चिमी महाराष्ट्र में अम्बेडकर के नेतृत्व में संचालित हुआ था। एक बड़ी तादाद में दलितों ने महाड के एक तालाब के पानी को इस्तेमाल करने पर लगी रोक को मानने से इंकार कर दिया। अपने सत्याग्रह के तहत वे एकजुट होकर आगे बढ़े और तालाब का पानी पिया। उसके बाद, रूढ़िवादी तबके के गुस्साए लोगों ने उन पर डंडों और गदाओं से हमले किये। अम्बेडकर ने, जो कि महाड में ख़ुद मौजूद थे, बुद्धिमानी से अपने लोगों से जवाबी हिंसा न करने की अपील की। गांधी ने हमले के वक़्त ‘दलितों के मानसिक संतुलन’ की तारीफ लिखकर की। दलितों के “अनुकरणीय आत्म- नियंत्रण” की तारीफ करते हुए गांधी ने लिखा कि तथाकथित रूढ़िवादी दल ने सरासर पशुवत बल का प्रयोग किया और उसके पक्ष में वो कोई सफाई नहीं दे सकते।
इससे बढ़कर गांधी ने 28 अप्रैल 1927 के यंग इंडिया में लिखा:
‘डॉ. अम्बेडकर इस मायने में बिलकुल ठीक थे कि उन्होंने बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल और महाड नगरपालिका के प्रस्तावों को यह कहकर परखा कि तथाकथित अछूत तालाब पर जाएँ और अपनी प्यास बुझाऐं। महात्मा ने छुआछूत का विरोध करने वाले हर हिन्दू से महाड के दिलेर दलितों का बचाव करने की सलाह दी, “भले ही” इस कोशिश में “सर फोड़ दिए जाने का जोखिम हो।’[vii]
याद कीजिये राउंड टेबल कांफ्रेंस में उन्होंने कहा था – ‘अस्पृश्यता के जीवित रहने की तुलना में मैं हिन्दू धर्म का मर जाना पसंद करूंगा।‘[viii]
इसी दौरे पर एक ब्रिटिश पत्रकार से उन्होंने कहा था –
मैं सबसे ग़रीब सफ़ाईकर्मी के सामने घुटनों पर झुक जाऊँगा, उसके पैरों की धूल भी ले लूँगा क्योंकि सदियों से हम उन्हें कुचलने के भागीदार रहे हैं, लेकिन कभी राजा के सामने नहीं झुकूँगा, प्रिंस ऑफ वेल्स तो चीज़ ही क्या हैं![ix]
फिर भी वैज्ञानिक नहीं थी जाति को लेकर उनकी आरंभिक समझदारी
हालाँकि, मुझे हमेशा लगता है कि प्राचीन या समकालीन इतिहास की गांधी की समझ अध्ययन पर कम और कल्पना तथा सुनी-सुनाई बातों पर अधिक आधारित थी जिसमें प्राचीन काल में सब महान था, गाँवों में आत्मनिर्भरता थी, शांति थी जैसी धारणाएँ बनी थीं। जिस बिंदु पर गांधी अटकते हैं वह है वर्णों की व्यवस्था में अधिकृत कामों में बदलाव से इंकार। वह श्रम के सम्मान की बात करते हैं और सफ़ाई के काम को छोटा न समझने की बात ही नहीं करते बल्कि अपने उदाहरण से यह साबित करने की बात करते हैं, लेकिन यह काम शूद्रों द्वारा ही क्यों किया जाए और ब्राह्मण इस काम को क्यों न करें, इसका उत्तर नहीं ढूंढ़ते।
मज़ेदार यह है कि 1857 पर लिखे अपने लेख में मार्क्स भी भारतीय गाँवों को आत्मनिर्भर ईकाई की तरह ही देख रहे थे। लेकिन न ही मार्क्स न गांधी उस आत्मनिर्भरता के परदे में छिपी उस भयावह शोषण की व्यवस्था को देख पा रहे थे जो वर्ण व्यवस्था के रूप में पल रही थी। मार्क्स दूर थे, अंग्रेज़ी अख़बारों पर निर्भर इसलिए उनका अपरिचय समझ आता है। गांधी तो बचपन में कथित अस्पृश्य जाति के बच्चे से खेलने के कारण डाँट सुन चुके थे और लगातार छुआछूत के ख़िलाफ़ थे, फिर वह गाँवों के भीतर इस श्रम विभाजन में छिपी वह व्यवस्था क्यों नहीं देख पा रहे थे जिसमें श्रम करने वालों को निचले पायदान पर भेज दिया गया था और एक बड़े हिस्से को अस्पृश्य बना दिया गया था, यह सवाल गांधी को पढ़ते बार-बार जेहन में आना स्वाभाविक है। सी.एफ. एंड्रयूज़ गांधी के वर्ण व्यवस्था के समर्थन और अस्पृश्यता के विरोध के द्वैत को डीकोड करते हुए कहते हैं-
जहाँ गांधी हिन्दुत्व की अपनी परिभाषा में घोषणा करते हैं कि वह जाति-व्यवस्था में भरोसा करते हैं, वह अस्पृश्यता को पूरी तरह से नकार देते हैं। वह यह भी नहीं स्वीकार करते कि कोई भी जाति, जैसे कि ब्राह्मण, दूसरी जातियों से श्रेष्ठतर है। वह सभी औरतों और मर्दों को बराबर मानते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में समान व्यवहार करते हैं।[x]
जातियों की व्यवस्था के रहते हुए उनके विभेद को ख़त्म किया जाना सुनने में एक आदर्श प्रस्ताव लग सकता है लेकिन अनुभव यही बतातें हैं कि ग़ैर बराबरी और उच्चानुक्रम इसकी मूल निर्मिति में अंतर्विन्यस्त हैं। गांधी ने इस बाबत लगातार अपने अख़बारों में लिखा है लेकिन फ़िलहाल विस्तार में गए बिना हम यह कह सकते हैं कि यह सवाल अपनी तरह से गांधी को भी मथ रहा था और ज़ाहिर था कि यह सवाल भारत में काम करते हुए लगातार उपस्थित था।
मार्च-1915 में अहमदाबाद के कोचराब में जब उन्होंने पहले आश्रम की स्थापना की तो वहाँ कोई नौकर नहीं रखा गया, सभी को काम करना था। यहाँ रहने के लिए जो प्रतिज्ञाएँ आवश्यक थीं उनमें अस्पृश्यता का अस्वीकार अंतिम प्रतिज्ञा ज़रूर थी लेकिन थी बेहद महत्त्वपूर्ण। जल्द ही इसके अनुपालन का समय आया जब सितम्बर के महीने में बम्बई के एक दलित जाति के शिक्षक दूदाभाई अपनी पत्नी दानीबेन और बिटिया लक्ष्मी के साथ आश्रम में रहने आए। गांधी ने उन्हें ससम्मान आश्रम में जगह दी तो रहवासियों के बीच बावेला मच गया। कस्तूरबा ने आश्रम छोड़ देने की धमकी दी।
गांधी ने कहा कि यह उनके लिए बेहद कष्टप्रद होगा लेकिन वह उन्हें रोकेंगे नहीं। या तो उन्हें नियम पालन करने होंगे या वह जा सकती हैं। तूफ़ान फ़िलहाल थम गया लेकिन बीच-बीच में उफान आते रहे। और यह विरोध आश्रम के भीतर ही नहीं सीमित था। अब तक आश्रम के संचालन के लिए खुले हाथ से मदद करने वाले अहमदाबाद के कपड़ा मिल मालिकों ने इसके बाद हाथ खींच लिए। गांधी अपने फ़ैसले पर अडिग थे और एक वक़्त ऐसा आया जब उनके पास पैसे एकदम ख़त्म हो गए। अचानक एक दिन आश्रम के सामने एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक आदमी निकलकर उनके पास आया, एक लिफ़ाफ़ा सौंपा और लौट गया। लिफ़ाफ़े में तेरह हज़ार रूपये थे।[xi]
अस्पृश्यता के विरूद्ध गांधी और पूना समझौता
तीस के दशक में डांडी मार्च से शुरू हुए असहयोग आंदोलन के बाद से ही उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन तेज़ कर दिया था। गांधी अस्पृश्यता को हिन्दू धर्म के अहिंसा के भाव के विरुद्ध मानते थे और कहते थे कि इसे ख़त्म न किया गया तो हिन्दू धर्म समाप्त हो जाएगा।[1]
यह रोचक है कि इस बिन्दु पर एक तरफ़ सनातनी हिन्दू उनसे नाराज़ रहे तो तो दूसरी तरफ़ डॉ.अंबेडकर की भी उनसे गहरी असहमति रही। अम्बेडकर की असहमति का मूल वे स्थितियाँ थीं जिनमें पूना समझौता हुआ।
17 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जिसके तहत दलित जातियों को सिखों, मुसलमानों, बौद्धों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इन्डियन समुदाय की तरह एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया और इस तरह पृथक निर्वाचन की सुविधा।[xii] अम्बेडकर इसे एक बड़ी जीत मानते थे जो दलितों को हिन्दू पक्ष से अलग एक स्वतन्त्र अस्मिता का दर्जा दे रहा था और जिसके तहत दलितों को अपना नेतृत्व चुनने का मौक़ा मिल रहा था।
उन दिनों पूना की येरवडा जेल में बंद गांधी ने इसका इस आधार पर विरोध किया कि दलित हिन्दू समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देना हिन्दुओं को बाँटने की साजिश है। वह गोलमेज़ सम्मलेन में अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके थे। उन्होंने प्रधानमन्त्री को ख़त लिखा कि अगर यह अवार्ड वापस नहीं लिया गया तो 20 सितम्बर की दोपहर से वह आमरण अनशन पर चले जाएँगे, प्रधानमंत्री से हुए पत्र व्यवहार में जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो गांधी तय तिथि से अनशन पर चले गए। पेन लिखते हैं कि गांधी ने इस उपवास को अस्पृश्यता विरोध के लिए जनता को झकझोरने के लिए इस्तेमाल किया।[xiii]
जेल में गांधी के उपवास शुरू होने से एक दिन पहले इलाहाबाद के बारह मंदिरों ने पहली बार अपने दरवाज़े दलितों के लिए खोल दिए। जिस दिन उपवास शुरू हुआ उस दिन कई बड़े और पवित्र मंदिरों ने उनका अनुकरण किया। जवाहरलाल नेहरू की बेहद रूढ़िवादी माँ स्वरूपरानी नेहरू ने, जिन्होंने उम्र भर पति और बेटे की प्रगतिशीलता से अपने चौके-चूल्हे को बचाए रखा था, दलितों के हाथ का खाना खाया। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति और अनेक ब्राह्मणों ने दलितों के साथ सहभोज का आयोजन किया। गाँवों-कस्बों में सहभोज आयोजित किये गए।[xiv]
कह पाना मुश्किल है कि इसमें कितने जेश्चर कॉस्मेटिक थे और कितनों का वास्तविक हृदय परिवर्तन हुआ लेकिन इसने देश भर में अस्पृश्यता विरोध की जिस बहस को जन्म दिया और जिस तरह का उसे समर्थन मिला वह उस दौर में सनातनियों को नाराज़ करने के लिए काफी था।
इस असर को चिह्नित करते हुए फिशर समाहार करते हैं –
यह अनशन अस्पृश्यता के तीन हज़ार वर्षों से अधिक के शाप को नहीं मिटा पाया। मंदिर में घुसना किसी बेहतर नौकरी में जाना नहीं है। हरिजन भारतीय समाज की तलछट पर ही रह गए। जब गांधी ने संतरे का जूस पीया तो वह बँटवारा समाप्त नहीं हो गया। लेकिन इस अनशन के बाद अस्पृश्यता को जो सामाजिक स्वीकृति मिली हुई थी वह ख़त्म हो गई। इसमें जो भरोसा था वह नष्ट हुआ। इसे नाजायज़ माना जाने लगा…सामाजिक रूप से दलितों से संपर्क रखना अनुचित माना जाता था, अब कई जगहों पर सामाजिक रूप से उनसे दूरी बनाना ग़लत माना जाने लगा। अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले को कट्टर और प्रतिक्रियावादी माना जाता था।[xv]
इधर अनशन ख़त्म कराने के लिए लगातार फ़ॉर्मूले निकालने की कोशिश शुरू हुई और जेल प्रांगण में ही कई बैठकें हुईं। गांधी तब तिरसठ के हो चुके थे और उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा अनशन झेल पाते। पेन लिखते हैं कि चुनावों के संदर्भ में अम्बेडकर जितनी मांग कर रहे थे गांधी से उससे अधिक का प्रस्ताव दिया था लेकिन अम्बेडकर अपने फ़ॉर्मूलों पर अड़े हुए थे।[xvi]
ज़ाहिर है वह कम्युनल अवार्ड खोने के बाद दलितों के राजनैतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व के लिए अधिक से अधिक सम्मानजनक शर्तें चाहते थे। अस्पृश्यता निवारण का एक प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता था लेकिन वह राजनैतिक प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकती थी। सैकड़ो वर्षों की ग़ुलामी के चलते दलित वर्ग जिन हालात में पहुँचा था उससे निकालने के लिए वह किसी की सदाशयता पर निर्भर नहीं रह सकते थे।
अंततः जो समझौता हुआ उसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो ख़त्म कर दी गई लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में अरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 और केन्द्रीय विधानमंडल में 18 प्रतिशत कर दी गई तथा संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई, साथ ही दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। ध्यान देने योग्य बात है कि गांधी ने दलितों को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व की बात की थी और यह अवार्ड में दी गई सीटों से अधिक संख्या थी।
इस समझौते पर दस्तख़त के तुरंत बाद अम्बेडकर ने कहा कि वो गांधी और अपने बीच ‘बहुत कुछ समान’ पाकर चकित थे; बुरी तरह चकित। अगर आप ख़ुद को पूरी तरह दलित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर देते हैं, अम्बेडकर ने गांधी से कहा, आप हमारे नायक बन जाएँगे।[xvii]
कोई बारह साल बाद अपने 1945 के अपने निबंध व्हॉट कांग्रेस एँड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में कई जगह अम्बेडकर दावा करते हैं कि उनके लिए पूना पैक्ट एक विजय थी।
वह आगे लिखते हैं कि “जब उपवास विफल हुआ और गांधी पैक्ट पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हुए– जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है और जो अछूतों की राजनीतिक मांगों को स्वीकार करता था—‘उन्होंने [गांधी ने] कांग्रेस को इन राजनीतिक अधिकारों को हासिल करना मुश्किल बनाने के लिए गलत चुनावी कार्यनीति अपनाने की छूट देकर अपना बदला ले लिया।’
ज़ाहिर है इस लेख में वह पूना समझौते की शर्तों की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि उसे लागू किये जाने में जो दिक्कतें हुईं उनकी बात कर रहे हैं।
इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ साइन्स के प्रोफ़ेसर उदय बालकृष्णन 14 अप्रैल 2020 को द हिन्दू लिखे एक लेख में कहते हैं –
पेरी एंडरसन और अरुंधती रॉय का तर्क है कि गांधी ने अपने उपवास से अम्बेडकर पर दबाव बनाया कि वह पूना समझौता करें, हालाँकि अम्बेडकर ऐसे आदमी नहीं थे जो किसी की इच्छा के सामने घुटने टेक दें। इस घटना के एक साल बाद ही वह बेहद स्पष्ट थे और उन्होंने कहा कि वह ऐसे किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसकी इच्छा और सहमति पर कोई समझौता आधारित हो…एक व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अम्बेडकर किसी परिपूर्ण समाधान की उम्मीद नहीं कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने 1943 में गोविन्द महादेव रानाडे के सौवें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘वह किसी तरह का एक बंदोबस्त चाहते थे और वह किसी आदर्श बंदोबस्त के लिए प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं थे। इसी भाव से उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।[xviii]
राजमोहन गांधी कहते हैं –
अम्बेडकर के 1945 के उस लेख का सन्दर्भ क्या था जो उन्होंने नयी दिल्ली के अपने पृथ्वीराज रोड स्थित सरकारी आवास पर लिखा था? इस वक़्त, वो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य थे। युद्ध लगभग ख़त्म होने वाला था और भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से, जिसने भारत के बड़े हिस्से में उथल- पुथल मचा दी थी, तीन साल जेल में रहने के बाद कांग्रेस नेतृत्व रिहा किया जाने वाला था। ब्रिटिश सरकार भारत के लिए एक नयी राजनीतिक योजना लाने के कगार पर थी और पूरे देश में नए चुनाव आने वाले थे।
एक प्रबुद्ध चिंतक और एक सदस्य (दरअसल मंत्री) के रूप में 1945 का यह लेख लिखते हुए वह किसी भी नई ब्रिटिश योजना को प्रभावित करना चाहते थे। साथ ही, वह एक राजनीतिक नेता भी थे जो 1937 चुनावों के परिणाम भूल नहीं सकते थे जो कि विश्व युद्ध के कारण इन चुनावों के पहले हुआ आखिरी चुनाव था। अब 1945-46 में वे बेहतर परिणामों की उम्मीद रखते थे। अपने 1945 के निबंध के मार्फ़त, 1937 के चुनाव परिणामों से बेचैन अम्बेडकर, ब्रिटिश नेताओं के सामने अपना पक्ष रख रहे थे और साथ ही भारतीय मतदाताओं के सामने भी।
हालांकि 1945 के चुनावों ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मतदाताओं में, जिसमें भारी तादाद में दलित भी शामिल थे, कांग्रेस को लेकर जबरदस्त आकर्षण था। उच्च जाति हिन्दुओं के साथ- साथ दलित वोट भी हासिल करते हुए कांग्रेस ने 1937 की तुलना में कहीं ज्यादा संख्या में दलित सीटें जीतीं।[xix]
राजमोहन गांधी 1932 के बाद गांधी के लगातार जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ होते जाने को चिह्नित करते हुए बताते हैं कि जहाँ
24 अप्रैल 1947 को उन्होंने पटना में कहा कि पिछले कुछ समय से उन्होंने “एक उसूल बनाया है कि वो उस विवाह में शामिल नहीं होंगे न ही उसे आशीर्वाद देंगे जिसमें कम-से-कम एक पक्ष हरिजन न हो” वहीं जून 1947 में उन्होंने किसी दलित और संभव हो तो दलित(मेहतर) स्त्री को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया था।[xx]
वह रेखांकित करते हैं कि गांधी अगर सीधे जाति-व्यवस्था पर प्रहार करते तो लोग उनके साथ नहीं आते इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था के सबसे कमज़ोर पक्ष, छूआछूत पर प्रहार कर इसे कमज़ोर करने की कोशिश की। वह इसबात को महसूस कर रहे थे कि बिना सामाजिक सुधारों के राजनैतिक सुधार हुए तो अंततः एक संवेदनहीन ब्रिटिश शासन की जगह उतने ही संवेदनहीन भारतीय शासन की स्थापना करेंगे।[xxi]
एक उदाहरण गांधी की जाति पर समझ का
गांधी जाति के सवाल को कैसे देख रहे थे, इसे समझने में मुझे 9 जून 1946 को लिखा उनका एक नोट बहुत काम का लगता है। वह लिखते हैं –
एक ब्राह्मण संवाददाता ने मुझसे इस तथ्य को प्रकाशित करने के लिए कहा कि वह हरिजन बन चुका है और सेंसस में भी ऐसा परिवर्तन कराना चाहता है। यह मेरी उस अपील का परिणाम था जिसमें मैंने सभी ऊँची जाति के हिन्दुओं से ख़ुद को कथित निचले तबके के हरिजन के रूप में देखने की अपील की थी।
लेकिन इस आतंरिक परिवर्तन को प्रचारित करने की क्या ज़रुरत है? परिवर्तित हुए व्यक्ति का वास्तविक सबूत इस परिवर्तन को अपने निजी जीवन में लागू करना है। इसके लिए वह आराम से भंगियों से हिलेगा-मिलेगा और उनकी ज़िन्दगी में सक्रिय भागीदारी करेगा। अगर संभव हो तो वह किसी भंगी के साथ ही रहेगा। वह अपने बच्चों की शादी हरिजनों से करेगा और वह कहेगा कि वह अपनी मर्जी से हरिजन बना है और सेंसस रजिस्टर में अपना नाम हरिजन या भंगी की तरह दर्ज कराएगा।
लेकिन यह सब करने के बाद भी वह हरिजनों के अधिकारों पर हक़ नहीं जमाएगा, उदाहरण के लिए वोटर लिस्ट में वह अपना नाम हरिजन के रूप में दर्ज नहीं कराएगा। दूसरे शब्दों में वह एक हरिजन के दायित्व पूरी तरह से निभाते हुए उनके लिए तय किसी अधिकार में हिस्सेदारी नहीं करेगा। जब तक अलग वोटर लिस्ट बनी हुई हैं वह वोटर नहीं रहेगा।[xxii]
इस परिघटना का ज़िक्र थोड़ा विस्तार से करना मुझे दो वजहों से ज़रूरी लगा। एक तो इसलिए कि इस दौर में तेज़ हुए अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन के चलते कई बार कहा जाता है कि असल में गांधी ने कम्युनल अवार्ड टालने के लिए यह आन्दोलन शुरू किया। दूसरे, यह गांधी के जीवन की एक अजीब त्रासदी को बताता है। सही या ग़लत यह आपकी पक्षधरता पर निर्भर करता है लेकिन तथ्य यह है कि यह करके उन्होंने दलितों को हिन्दू धर्म से अलग एक अस्मिता के रूप में बाँटने को रोका और उन्हें सनातनियों से हिन्दू विरोधी होने का आक्षेप झेलना पड़ा।
यह हिस्सा मेरी किताब ‘उसने गांधी को क्यों मारा‘ से
[1] अस्पृश्यता पर गांधी के विचार और विस्तार से जानने के लिए पाठक नवजीवन पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित उनकी पुस्तक द रिमूवल ऑफ़ अनटचेबिलिटी पढ़ सकते हैं.
[i]देखें, पेज 160-61, इंटरटेनिंग गाँधी, मुरियल लिस्टर, रिचर्ड क्ले एंड संस लिमिटेड, लन्दन -1932
[ii]देखें, पेज 280, द एसेंशियल गाँधी, (सं) लुई फिशर, रैंडम हाउस, न्यूयार्क-1962
[iii]देखें, वही, पेज 181-82
[iv]देखें, वही, पेज 285,
[v]देखें, पेज 47-48, इंटरटेनिंग गाँधी, मुरियल लिस्टर, रिचर्ड क्ले एंड संस लिमिटेड, लन्दन -1932
[vi]देखें, पेज 139, खंड 16, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ महात्मा गाँधी, गाँधी सेवाग्राम आश्रम, वर्धा -1999
[vii]देखें राजमोहन गाँधी का लेख, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय : अम्बेडकर-गाँधी विमर्श, https://swaadheen.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html?m=1
[viii]देखें, पेज 439 , द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गाँधी, रॉबर्ट पेन, रूपा, दिल्ली -1997
[ix]देखें, पेज 40, इंटरटेनिंग गाँधी, मुरियल लिस्टर, रिचर्ड क्ले एंड संस लिमिटेड, लन्दन -1932
[x]देखें, पेज 29, महात्मा गाँधीज़ आइडियाज़, सी एफ एंड्रयूज, तीसरा संस्करण, हेंडरसन एंड स्पालडिंग, लंदन -1949
[xi]देखें, पेज 294 , द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गाँधी, रॉबर्ट पेन, रूपा, दिल्ली -1997
[xii]देखें, पेज 439 , द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गाँधी, रॉबर्ट पेन, रूपा, दिल्ली -1997
[xiii]देखें, वही, पेज 442 ,
[xiv]देखें, पेज 280, द एसेंशियल गाँधी, (सं) लुई फिशर, रैंडम हाउस, न्यूयार्क-1962
[xv]देखें, वही, पेज 281
[xvi]देखें, पेज 434 , द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गाँधी, रॉबर्ट पेन, रूपा, दिल्ली -1997
[xvii]राजमोहन गाँधी के पूर्वउद्धरित लेख, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय : अम्बेडकर-गाँधी विमर्श में उद्धरित
[xviii]https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/ambedkar-and-the-poona-pact/article31333684.ece (आख़िरी बार 01.08.2020 को देखा गया)
[xix]https://swaadheen.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html?m=1 (आख़िरी बार 01.08.2020 को देखा गया)
[xx]देखें, पेज 3, महात्मा : लाइफ ऑफ़ मोहनदास करमचंद गाँधी, खंड 8, डी जी तेंदुलकर, विट्ठलभाई के जावेरी और डी जी तेंदुलकर, बम्बई- 1954
[xxi]देखें, पेज 175, गाँधीज़ पैशन, स्टेनली वोलपर्ट, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क – 2001
[xxii]देखें, पेज 139, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी, खंड 91 ( गाँधी आश्रम सेवाग्राम द्वारा प्रकाशित)

मुख्य संपादक, क्रेडिबल हिस्ट्री