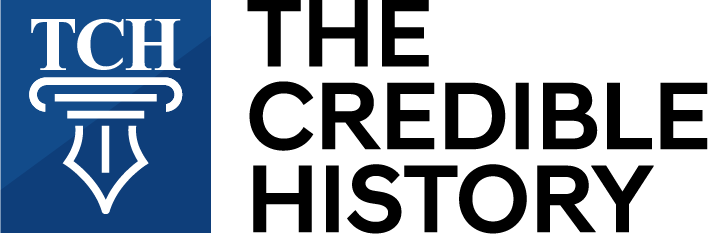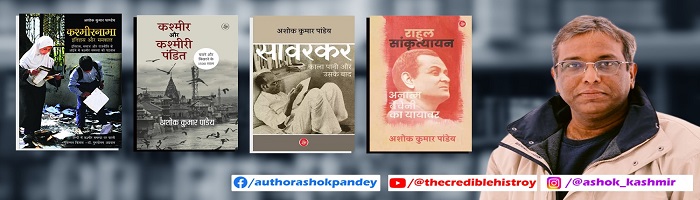CapitalismFeaturedMarxPeople's History
प्रिय पूंजीवाद, मार्क्स अभी अप्रासंगिक नहीं हुये है
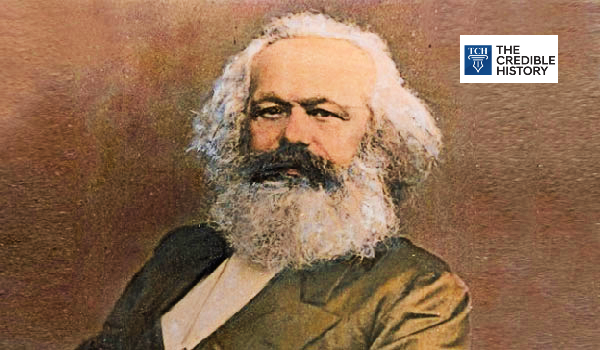
मार्क्स यदि जीवित होते तो 5 मई 2018 को 202 वर्ष के हो गए होते। तो क्या? क्या मार्क्स के विचारों को याद करने और उन पर चिंतन करने से अब कोई फायदा है ? क्या यह एक तथ्य नहीं है कि पूंजीवाद ने मार्क्सवाद द्वारा बुरी तरह पछाड़ दिया है। क्या यह एक तथ्य नहीं है की स्वयं आज वामपंथी बुद्धिजीवी “वर्ग” की जगह “पहचान” की तरफ अधिक झुके हुये है, इतिहास की जगह “संस्कृति” से ज्यादा सरोकार रकते है, और “सार्वभौम मूल्यों” की तुलना मे “विभेदों” की उपस्थिती मे ज्यादा विश्वास रखते है।
क्या इतिहास ने स्वयं यह निर्णायक फैसला नहीं कर दिया है की मार्क्स अब प्रासंगिक नहीं रह गए है? क्या साम्यवादी शासन भयावह रूप से दमनकारी नहीं रहे है और क्या मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टियां समकालीन विश्व और उसकी समस्याओं, मुद्दों से कटी हुई नहीं है?
सारांश यही है की 21वीं सदी बिना किसी बड़े बौद्धिक जोखिम के मार्क्स को अनदेखा कर सकती है; या ज्यादा से ज्यादा, कोई महत्व दिये बिना बस एक औपचारिक जिक्र कर आसानी से आगे बढ़ सकती है।
मार्क्स-एक मानव, न कि पैगंबर
लेकिन ऐसा करना भारी भूल होगी । मार्क्स को लेनिन, स्टेलिन, माओ या किसी अन्य मार्क्सवादी के अच्छे-बुरे कृत्यों के लिए उत्तरदाई ठहराने का कोई मतलब नहीं है। उनका मूल्यांकन उनकी अपनी राजनित्क गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, और किया भी गया है, लेकिन मार्क्स के दशकों बाद आने वाले लोगों की राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हे को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं।
फिर, यह भी नहीं भूलना चाहिए की मार्क्स कोई पैगंबर नहीं थे जो कोई गलती न कर सके। वे बेशक कई मामलों मे गलत थे, लेकिन फिर भी मार्क्स एवं फ़्रेडरिक एंजेल्स और “भौतिक परिस्थितियों” की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे मे उनकी सूक्ष्मदृष्टि हमे इतिहास के उतार-चढ़ावों और मानव जीवन के मूलभूत मुद्दों और समस्याओं को समझने मे काफी मदद कर सकती है।
यदि मार्क्स से अपने परवर्तियों के कृत्यों के उस बोझे को हटा लिया जाये जो उनपर जबर्दस्ती लाद दिया गया है, तो मानव स्वभाव के बारे मे मार्क्स की समझ और पूंजीवाद के बारे मे उनकी अंतर्दृष्टि बहुत प्रासंगिक है और हम उनसे काफी कुछ सीख सकते है। लेकिन यह सीख मार्क्स का ज्यों का त्यों अनुरसरण करना नहीं हो सकती ।आज हमे मार्क्स से सिर्फ अंतर्दृष्टि की ही उम्मीद करनी चाहिए, आज की परिस्थ्तियों के लिये पहले से तैयार समाधानों की नहीं।
पूंजीवाद और मानवता की निराशा
20वी सदी सपनों और आशाओं के टूटने और निराशा एवं दुःस्वप्न मे बदलने की सदी थी। न सिर्फ साम्यवाद बल्कि कई अन्य देवताओं ने मानवता को धोखा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ की किसी सार्वभौमिक महत्व के ग्रांड नरेटिव की बात करना भी राजनीतिक दृष्टि से गलत समझा जाने लगा।
लेकिन साथ ही, मानव चेतना की समस्या महामारी का रूप ग्रहण करने लगी है। सबसे ज्यादा सफल माने जाने वाले पूंजीवादी देश –अमरीका मे “मन की शांति” प्रदान करने वाले पोंगा पंडितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहाँ मनोचिकित्सा के व्यवसाय का भी दिनों दिन विस्तार हो रहा है।अधिकांश अमरीकी अवसाद दूर करने की दवाओं को लेने के लिए मजबूर है। ऐसा लगता है मानो सामाजिक सम्बन्धों का टूटना “विकास” की पूर्वशर्त बन गया है; आज हमारा अपना समाज इसका उदाहरण है।
गांधीजी इस खतरे को अपने अंदाज मे पहले ही भाप चुके थे, और नेहरू जी भी, जैसा की उन्होने 1960 मे आर॰के॰ करांजीया को बताया था, “हमारी तकनीकी सभ्यता के आध्यात्मिक खोखलेपन” के प्रति चिंतित थे ।
मानवता का ह्रास, मानव होने के एहसास का खो जाना –मानव स्वभाव से अलगाव –मार्क्स के जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी। 30 वर्ष से भी कम की आयु मे लिखी उनकी “इकोनोमिक एंड फिलोसोफ़िकल मेन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844” मे मार्क्स ने मनुष्य को सोशल-बीइंग ही नहीं उस से भी बढ़कर “स्पीसीज़ बीइंग” बताते हुए, मानव के इसी पहलू का सार पकड़ने का प्रयास किया है। इन नोट्स मे मार्क्स लुडविग फ्यूअरबेक और हिगल से प्रभावित थे।
मार्क्स मनुष्य की “अद्वितीयता” को रेखांकित करते है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य महज प्रकृति का जैविक विस्तार नहीं है; वह प्रकृति मे है और, अन्य प्राणियों से भिन्न, वह इस बात को जानता भी है। अपने होने की इस चेतना से मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध अन्य प्राणियों के प्रकृति के साथ संबंध की तुलना मे गुणांत्मक रूप से भिन्न हो जाता है। मार्क्स ने स्वयं इस संबंध को “अजैविक, आध्यात्मिक(स्प्रिच्यूअल)” (मार्क्स के स्वयं के शब्दों का हिन्दी अनुवाद) कहा है ।
जब मनुष्य की स्वाभाविक शारीरिक-मानसिक गतिविधि को बाजार मे बिकने वाली वस्तु बना दिया जाता है तो उसका अपने ही उपरोक्त आध्यात्मिक पक्ष से अलगाव हो जाता है। अलगाव की यह प्रक्रिया सामाजिक संगठन की शुरुआत से शुरू हो जाती है जो पूंजीवाद मे पहुच कर एक भयावह रूप धरण कर लेती है। पूंजीवाद मे मनुष्य का बाह्य-प्रकृति और उसके अपने आध्यात्मिक पक्ष से ही नहीं, स्वयं अपने शरीर तक से अलगाव हो जाता है।
धर्म बतौर दर्द-निवारक
मार्क्स ने संस्थागत धर्म पर भी इसी दृष्टि से विचार किया है। मार्क्स ने बताया कि धर्म “मानव कल्पना की स्वतःस्फूर्त गतिविधि” से मनुष्य का अलगाव कर उसके स्थान पर दैवीय-पिशाचीय के चिंतन को स्थापित कर देता है। साधारण शब्दों मे धर्म विश्व के साथ एकत्व महसूस करने की भावना को, ब्रह्मांडीय-आश्चर्य को और चेतना की अभिव्यक्ति को एक बाहरी वस्तु का रूप दे देता है।
https://thecrediblehistory.com/leaders/others/international/history-of-may-day/
मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम कहा है । मार्क्स की यह उक्ति जितनी प्रख्यात है उतनी ही ज्यादा गलती इसे समझने मे हुई है। अफीम से मार्क्स का तात्पर्य नीद की दवा या दर्द निवारक से है जो विध्यमान परिस्थितियों के कारण जरूरी हो गई है। जैसे ही इस संदर्भ मे मार्क्स का पूरा कथन पढते है यह बात बिलकुल साफ हो जाती है-“धार्मिक-पीड़ा, वास्तविक पीड़ा की अभिव्यक्ति भी है और साथ ही साथ उस वास्तविक पीड़ा का विरोध भी। धर्मं शोषित व्यक्ति के लिए राहत की सांस का काम करता है, वह हृदयहीन विश्व का हृदय है, आत्माहीन-अमानवीय परिस्थितियों की आत्मा है। धर्म जनता के लिए अफीम है”।
कालांतर मे मार्क्स ने “आध्यात्मिक (स्प्रिच्यूअल)” जैसे शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया और अपने विचारों को अधिक सेकुलर शब्दावली मे प्रस्तुत किया, किन्तु अब भी उनकी चिंता वही अलगाव ही था। अपनी सबसे प्रख्यात कृति “केपिटल” मे मार्क्स पूंजीवाद की कठोर निंदा इसलिए की है कि वह श्रमिक को बहुआयामी मनुष्य से गिराकर मशीन का ही एक अनुलग्नक मात्र, महज मजदूर, मे तब्दील कर देता है, उसके श्रम को “पीड़ा” मे बदल देता है और उसके जीवन-जीने-के-समय को काम-करने–के-समय मे बदल देता है जिसकी वजह से श्रमिक अपनी बौद्धिक शक्यता से दूर हो जाता है ।
गलत भविष्यवाणियाँ या गलत समझ ?
कुछ लोग मार्क्स की अप्रासंगिकता का प्रमाण उनकी इस भविष्यवाणी के सच नहीं होने मे देखते है कि “पूंजीवाद मे दिनों-दिन गरीबी बढ़ती जाएगी और मजदूरों की दशा खराब होती जाएगी”। यह सच है कि मार्क्सोत्तर पश्चिम मे पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर भी मजदूर समृद्ध हुये है। बस समस्या यह है की यदि विश्व अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप मे देखा जाये तो, पूंजीवादी व्यवस्था मे पश्चिम के मजदूरों की तरक्की की भयावह और घिनौनी कीमत पश्चिमेत्तर विश्व के लोगों ने चुकाई है, और आज भी चुका रहे है।
ब्रिटेन के श्रमिक इसीलिए ‘समृद्ध’ हो सके क्यों की अंग्रेजों ने भारत का सोचे-समझे तरीके से वि-औध्योगीकरण किया और गरीब बनाया; अमरीकी श्रमिक विश्व के विभिन्न हिस्सों मे “एक्सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी” के नाम पर पर थोपे गए शोषण के बिना समृद्ध नहीं हो सकता। यहाँ तक की भारत,चीन जैसे उन देशों मे जो विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे है वहाँ भी शहरों और उनके निवासियों को स्मार्ट बनाए जाने की कीमत दूसरे लोग चुका रहे है । ये लोग कहीं गायब नहीं हुये है, बस दिखना बंद हो गए है क्यों की मीडिया और बुद्धिजीवियों ने इनकी ओर आँख मूँद ली है।
बड़ी बड़ी कंपनियो के तथाकथित ‘बिजनेस प्रेक्टिसेज’ से तो सभी भली भांति परिचित है। वालमार्ट स्टोर्स मे सेल्स्पर्सन को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी जाती है, उनसे यह अपेक्षित है की वे 8-10 घंटे खड़े रहें।
सामान्य तौर पर कहा जाये तो आज नियमित रोजगार का स्थान “संविदा मजदूरों” और “आकस्मिक एवं अस्थायी कामगारों” (प्रबंधन शब्दावली मे “जस्ट इन टाइम”) ने ले लिया है । ‘पकोड़ा और पान की अर्थव्यवस्था’ इसी सोच का देशी अवतार है । नैतिकता से असंपृक्त मुनाफाखोरी के लिए जरूरी है की जितना संभव हो सके उतने लोगों को कल की रोजी-रोटी के लिए असमंजस मे रखा जाये । याद है किस प्रकार बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने मनरेगा का इसलिये विरोध किया था की इसकी वजह से ‘सस्ता श्रम’ ‘महंगा’ हो गया है और श्रमिक मिलने मे कठिनाई आ रही है ।
रोजी की यह अनिश्चितता चिंता और क्रोध को जन्म देती है जिसे या तो आक्रामक राजनीति की तरफ मौड़ दिया जाता है या फिर फर्जी ‘अध्यात्म’ या ‘मनोचिकित्सा’ की तरफ । और फिर, जैसा की मार्क्स ने कटाक्ष पूर्वक कहा था, “अपराधी सिर्फ अपराध को ही जन्म नहीं देते, बल्कि इससे निपटने के लिए जरूरी कानूनी ढांचे को भी जन्म देते है”।
https://thecrediblehistory.com/featured/women-labour-and-may-day/
आध्यात्मिक संकट, पूंजीवादी जड़ें
विश्व अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप मे देखने पर मार्क्स अप्रासंगिक और पुराने नहीं दिखाई देते है खास तौर पर जब वे कहते है –“एक सिरे पर धन का संकेन्द्रण उसी समय दूसरे सिरे पर दुख, श्रम की पीड़ा, दासता, अज्ञानता, अमानवीयता और नैतिक अवमूल्यन का संकेन्द्रण है”।
वे मार्क्स ही थे जिनहोने अपने मित्र एंजेल्स के साथ मिलकर ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ (1948) मे पूंजी की वैश्वीकरण की तरफ यात्रा की और बढ़ी बड़ी कंपनियों के विश्व के वास्तविक शासक बन जाने की –डेमोक्रेसी को कोर्पोरेटोक्रेसी द्वारा -बदल दिये जाने की भविष्यवाणी की थी।
आप इसे आध्यात्मिक कहे या कुछ और नाम दे, लेकिन अलगाव द्वारा पैदा हुये संकट को नकारा नहीं जा सकता ।मार्क्स ने इस संकट के “भौतिक” आधार और “ऐतिहासिक” परिप्रेक्ष्य को उजागर कर बहुत महत्वपूर्ण सेवा की है । सनद रहे, भौतिकवाद सुखवाद (नैतिकता से असंपृक्त सुख प्राप्ति की अंधी दौड़ ) नहीं है । बल्कि मार्क्सवादी भौतिकवाद सुखवाद की कड़ी आलोचना करता है।
जब कबीर अपनी एक कविता मे भीतर और बाहरी (‘भीतर बाहर शबद निरंतर’) की सतत अन्तरक्रिया की बात करते है तब वे परंपरागत भारतीय समझ को ही दोहराते है जो सही और गलत की एकांतवादी सोच के शिकंजे को खारिज करता है। जब मार्क्स इस बात पर ज़ोर देते है की मानव चेतना और भोतिक परिस्थितियाँ एक दूसरे पर द्वन्द्वात्मक रूप से कार्य करती है तो वे भी अपनी दार्शनिक परंपरा की शब्दावली मे, अपने तारीक से यही करते है।
‘आधात्मिक सुनेपन’ की समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी है की उत्पादन और वितरण की सारी व्यवस्था का मानवीयकरण हो। ‘आत्मा के संकट’ का इलाज महज आध्यात्मिक या मनोचिकित्सकीय उपायों से नहीं किया जा सकता। इसके समाधान हेतु भीतर चेतना की तरफ किये जाने वाले इस उपायों के साथ-साथ बाहरी की, जगत की समस्याओं का न्यायपूर्ण समाधान खोजना आवश्यक है।

जाने माने विद्वान। साहित्यालोचक और इतिहासविद