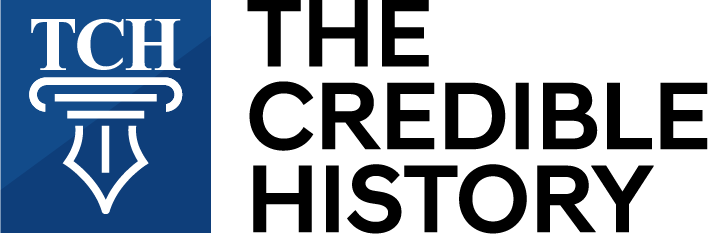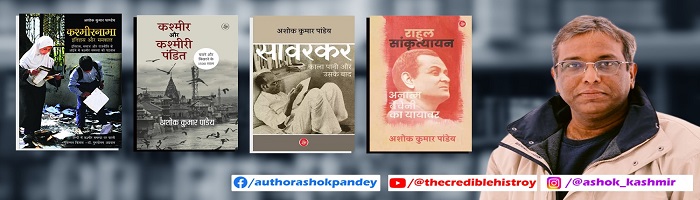पसमान्दा मुसलमान के दर्द की जड़ यहां है
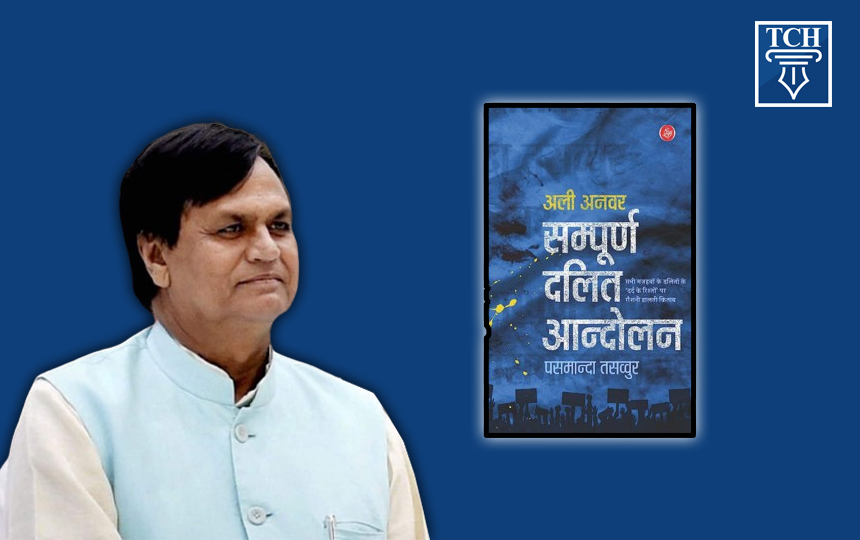
पसमान्दा मुसलमान और उनके दु:ख-दर्द को लेकर अरसे से संघर्ष कर रहे भूतपूर्व सांसद, पत्रकार, लेखक और जुझारू नेता अली अनवर साहब की महत्वपूर्ण किताब संपूर्ण दलित आन्दोलन –पसमान्दा तसव्वुर, हमारे जातिग्रस्त समाज से इंसाफ़ मांगती है। पेश है उनकी किताब का एक छोटा सा अंश-

हम सवाल करते, जवाब पाते और ख़ुद नये सवालों से घिर जाते
हम चले थे बच्चों – दलित मुसलमानों बच्चों – को देखने। सब गुलाब से लगे- लाल, पीले, काले गुलाब। बिहारी घर-समाज के और बच्चों जैसे। उनसे मिले, उनको छुआ, तो कांटे चुभे। तब महसूस हुआ कि ये तो कुछ अलग ही तरह के बच्चे हैं। बिखरे-मुरझाए, लेकिन इनको डाली से टूटे गुलाब नहीं कह सकते।
हमें बोध हुआ कि बच्चों को उनके परिवार के केन्द्र में रखकर ही जाना-समझा जा सकता है, ख़ासकर इन बच्चों की सही पहचान के लिए इनके परिवारों को देखना-समझना होगा और परिवार की सही पहचान तब तक सम्भव नहीं, जब तक उस समुदाय को न देखा-परखा जाए, जिससे परिवार जुड़ा है!
यहां तक सब ठीक रहा। हमने अपने बोध के मुताबिक़ प्रश्नावली तैयार की। अध्ययन-सर्वेक्षण शुरू हुआ। राजधानी पटना के विभिन्न दलित मुस्लिम बच्चों और इनके परिवारों के बीच पहुंचे। ख़ूब हंगामा हुआ। हम सवाल करते, जवाब पाते और ख़ुद नये सवालों से घिर जाते।
https://thecrediblehistory.com/featured/haar-kar-bhi-kabhi-nahi-hare-vaale-kuvar-singh-kbhai-amar-singh/
बच्चों को बच्चे की नज़र से देखना हो हमने सीखा ही नहीं!
हमारे सीधे-साधे सवालों के जवाब में अभिभावकों ने अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ कहा। कुछ दो टूक, तो कुछ चौकानेवाले जवाब।
जब हमने बच्चों से सवाल किए तो जवाब में हमारे हाथ आई उनके सूखे चेहरों से छलकती मासूम हंसी और बड़ों की बनाई दुनिया को पहचानने की कोशिश करती निश्छल-निर्दोष नज़रे! तब हमें एहसास हुआ कि हम तो बड़े ही नज़र से बच्चों को दिख रहे हैं, बच्चों को बच्चे की नज़र से देखना हो हमने सीखा ही नहीं!
बहरहाल, हमने अध्ययन-सर्वेक्षण जारी रखा। परिवार के बड़ों से सुना और बच्चों की नज़रों और हंसी को पढ़ने की कोशिश की। शुरु से हम बड़ों के दिमाग में बात थी कि दलित मुसलमान परिवार उच्च शिक्षा न सही, प्राथमिक शिक्षा के लिए तो अपने बच्चों को मदरसों और सरकारी स्कूल में ज़रूर भेजने होंगे।
लेकिन बच्चों के बीच जाकर पता चला कि प्राथमिक शिक्षा की उम्र से ये बच्चे कमाना सीखते हैं। ख़ुद-ब-ख़ुद कमाई सीखने का उनका ज़रिया होता है- रद्दी काग़ज और चीथड़े चुनना, बर्तन-बासन करना, पंक्चर साटना वग़ैरह-वग़ैरह।
यह वेबसाईट आपके ही सहयोग से चलती है। इतिहास बदलने के खिलाफ़ संघर्ष में
वेबसाइट को SUBSCRIBE करके
भागीदार बनें।
पढ़ कर क्या नौकरी कहां मिलती है? ऊपर से बच्चा इतना काहिल हो जाता है
मां-बाप से पूछने पर कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते, जबकि वहां पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं लगती है, तो टका सा जवाब मिला- पढ़ाकर क्या करेंगे? नौकरी कहां मिलती है? ऊपर से बच्चा इतना काहिल हो जाता है कि उससे मोटा काम नहीं होता।
मज़हबी तालीम के लिए मदरसा भेजने की बाबत पूछने पर तो तंज़िया लहज़े में जवाब मिला- हमें अपने बच्चों को भिखमंगा थोड़े न बनाना है? इतना कहकर एक आदमी झट से चला गया। हम कहते रहे- अरे, रुको-रुको। इसका क्या मतलब है? वह रुका नहीं मानो कह रहा हो, मतलब निकालते रहे, अपने को बतखूच्चन के लिए फ़ुर्सत नहीं।
मदरसों से मुफ्त खाना मिलता है। सरकारी स्कूलों में भी आजकल मिड डे मील के नाम पर कभी-कभार कुछ मिल जाता है। भाई उस्मान हलालख़ोर और नूरहसन पंवरिया, जिन्हें साथ लेकर हम दलित मुसलमान बस्तियों में गए थे से हम घंटो बात-विचार किया कि खाना खिलानेवाले मदसरों में जाने से भला बच्चे भिखमंगे कैसे बन जाते हैं?
खूब माथा-पच्ची करने के बाद आखिर बात समझ में आई कि पहले मदरसों के बच्चे घरों से मुठिया वसूलते थे। इसकी जगह अब बच्चों के हाथ में चन्दे की रसीदें थमा दी जाती हैं या गमछा फैलाकर कुछ बटोर काने को कहा जाता है।
पहले कभी मदरसों से हर तबके के बच्चे पढ़ते रहे होंगे, अब यहां नीच दलित और पसमान्दा तबकों के बच्चे ही आते हैं। जिस बच्चे को कम उम्र में ही हाथ पसारने की आदत लगा दी जाए, वह एहसासे क़मतरी का शिकार होकर भिखमंगा नहीं तो क्या बनेगा?
जिस परिवार के गरीब होकर भी भिखमंगी क़बूल नहीं, वह अपने बच्चों को मदरसा क्यों भेजे? शायद यही सवालिया मतलब रहा होगा, उस चलते बने आदमी के जवाब का।
संदर्भ
अली अनवर, सम्पूर्ण दलित आन्दोलन, पसमान्दा तसव्वुर, राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2023
जनता का इतिहास, जनता की भाषा में