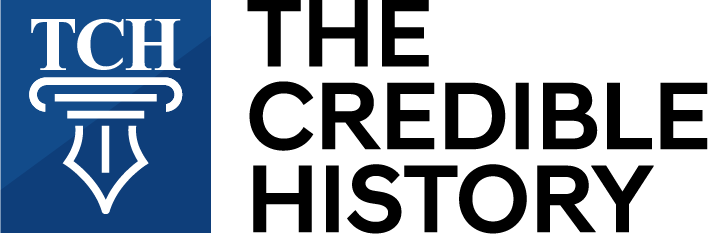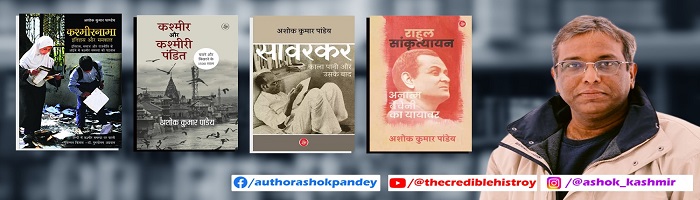दिल्ली की कहानी – सोहेल हाशमी की ज़ुबानी [Episode -2]

[जाने-माने हेरिटेज एक्टिविस्ट सोहेल हाशमी दिल्ली के शहर बनने की कहानी के साथ बात रहे हैं कि आखिर ‘शहर कैसे बनते हैं?’। पढिए इसकी दूसरी क़िस्त। ]
सो पिछली कड़ी के अंत में हम ने यह निवेदन किया था कि दो चीज़ों के साथ आने से कोई गाँव, बस्ती या आबादी शहर बन जाती है और वो दो चीज़ें हैं एक तो दूसरे लोगों का बाहर से आकर उस इलाक़े में बस जाना और दूसरा बाहर वालों और उस इलाक़े के लोगों के बाहर वालों के साथ होने वाले लेन-देन, यह लेन-देन व्यापार की शक्ल में भी होता है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की शक्ल में भी।
व्यापार से एक वर्ग विशेष का ही भला होता है मगर सांस्कृतिक आदान-प्रदान से एक ऐसे नज़रिये या दृष्टिकोण का विकास होता है जो नई जीवन-शैली, नए भोजन, नए पहनावे नए संगीत, नए शिल्प, नए औज़ार, नए साहित्य और नई भाषाओं से रू-ब-रू होना सीखता है, एक ऐसी संस्कृति का जन्म होता है जो इस सबकुछ नए से कुछ लेती है, कुछ उन्हें अपना देती है और इस तरह संसार की विभिन्नता से परिचित होती है।
परिचित होने के बाद धीरे-धीरे इस भिन्नता को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। भिन्नता को स्वीकारना एक गाँव के शहर बनने की यात्रा का बहुत महत्त्वपूर्ण क़दम है।
हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस बात का ज़िक्र करते चलें कि भिन्नता को स्वीकार करना कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है और इसलिए जो तीसरी चीज किसी जगह को गाँव से शहर बनाती है, उसका नाम है समय। वक़्त। कम से कम कुछ सौ बरस चाहिए होते हैं किसी आबादी को को शहर बनाने के लिए। तो अब समय, आदान प्रदान और प्रवासियों का आ कर बसना, गाँव को शहर बनने वाली तीन बुनियादी शर्तें हुईं।
शहर और क़स्बा
शहर, और शहर से हमारा अभिप्राय क़स्बा नहीं है, शहर वो है जहाँ दसियों लाख लोग आबाद हों, और दुनिया के सारे बड़े शहर ऐसे ही हैं, किसी भी शहर को देख लीजिए वहाँ कोई मूल निवासी नहीं मिलेगा, मूल निवासी गाँव में होते हैं, शहर प्रवासी ही बनाते हैं।
अब दिल्ली को ही ले लीजिए, अगर दिल्ली में से सारे प्रवासी निकाल दिए जाएँ तो क्या शहर बचेगा। बहुत से पुराने गाँव अलबत्ता बच जाएंगे, जाटों के गाँव, गूजरों के गाँव, कुछ गाँव सैनियों के, कुछ बस्तियाँ ब्राह्मणों की, कुछ दलितों की दूर-दूर फैली हुईं, खेतों से घिरी बस्तियाँ। इस इलाक़े को सैकड़ों बरस में शहर बनाया बाहर से आने वालों से।

बाहर से आने वालों का सिलसिला नया नहीं है
जब से दिल्ली के बारे में लिखित साक्ष्य हमें मिलने शुरू हुए हैं, बल्कि उस से थोड़े पहले से ही दिल्ली के जिन राजाओं के नाम हमें मिलते हैं वो संभवतः दिल्ली के नहीं थे, उन्होंने इस इलाक़े को जीता और यहाँ राज किया, और जब वो हार गए तो उन्हें हराने वालों ने यहाँ राज किया।
पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी, हरियाणा में स्थित तराईन के दूसरे युद्ध में वो एक अफ़गान मोहम्मद गौरी की फौज से दिल्ली हार गए। ग़ौरी ने अपने एक तुर्की ग़ुलाम क़ुतुब-उद-दीन ऐबक को आज़ाद करके अपना सूबेदार बना दिया। क़ुतुब-उद-दीन ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अपने एक ग़ुलाम इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी बनाया, इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया।
इस लंबी कहानी का हमारी बात-चीत से क्या रिश्ता है?
ज़रा सोचिए, ये शहर जिसमें पहले से ही आसपास के हरियाणवी, ब्रज, डोगरी, पंजाबी, मेवाड़ी , हड़ौती, मारवाड़ी बोलने वाले, व्यापारी फ़ौज़ी, कारीगर वगैरा पहुँच चुके थे अब यहाँ तुर्की, पश्तो, दरी, फ़ारसी बोलने वाले भी आने और बसने लगे और यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। कभी कम रफ़्तार से कभी बहुत तीव्र गति से।

विभाजन की अफ़रातफ़री
1947 में दिल्ली की आबादी 9 लाख थी, विभाजन की उथलपुथल, मार काट और लाखों लोगों के पाकिस्तान चले जाने की वजह से पहले तो यह आबादी 6 लाख रह गई और फिर चंद महीनों में 14 लाख हो गई। दिल्ली की भाषा, खाना, परिधान सब बदल गया। 1970 के दशक के अंत से यूपी और बिहार के भोजपुरी बोलने वाले इलाक़े और उसके आसपास के क्षेत्र से बहुत आबादी बड़ी संख्या में प्रवासियों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक़्त पूर्वांचली लोग दिल्ली की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं।
शहर ऐसे ही बनते हैं, जो भी दिल्ली में काम करके अपना पेट पालता है वो दिल्ली वाला है। और दिल्ली के कॉस्मोपोलिटन होने का सबसे बड़ा सबूत है कि आजतक दिल्ली में मूल निवासियों के लिए अलग अधिकारों की मांग नहीं उठी है।
जो लोग ये मांग कहीं भी उठा रहे हैं, उन्हें यह मानना होगा कि यह रवैया क़स्बाती समझ का नतीजा है, शहराती समझ का नहीं।
पहली क़िस्त : दिल्ली की कहानी – सोहेल हाशमी की ज़ुबानी

जाने-माने हेरिटेज एक्टिविस्ट, दिल्ली के इतिहास पर विशेष काम।