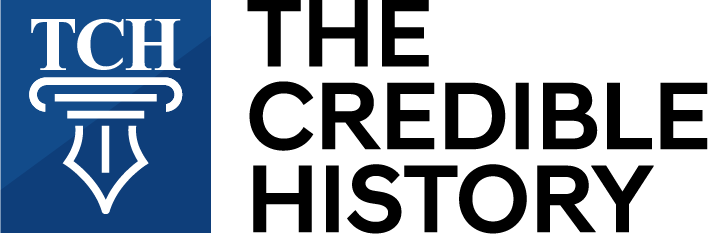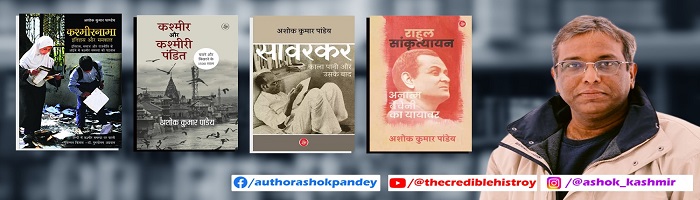निंदा और भक्ति से परे गांधी
गांधी पर बात करते हुए दो गलत रास्ते पकड़ना सबसे आसान है। एक भक्ति, दूसरा निंदा। मैं सोचती हूँ कि महात्मा की पदवी उन्हें भली ही लगती होगी। उसका जो दबाव बाकियों पर था उससे ज़्यादा गांधी पर खुद रहा होगा। दक्षिण अफ्रीका में मिली प्रसिद्धि के बाद जब वे भारत आए तो एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन चला पाना उनकी पहली बड़ी सफलता थी।
एक ऐसा काम था यह जिसके बारे में उस वक़्त ज़्यादातर प्रभावशाली लोग शंका में थे। यह व्याव्हारिक भी है या नहीं? यही गांधी की सबसे बड़ी ताकत बनी। अव्यावहारिक को व्यावहारिक बना देना। लोगों को अपने साथ ले आना। उन्हें नेतृत्व देना। उन्हें वह रास्ता दिखाना जो सत्ता के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष के लिए शायद सबसे उपयुक्त था उस वक़्त। अहिंसा और सत्याग्रह। आपको पता है कि आपके पास ताकत नहीं है, ऐसे में सत्ताधारियों के भीतर वह उदारता और करुणा जगाना कि वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करे इसके लिए सत्याग्रह और अहिंसा औजार भी थे, कवच भी।
लेकिन गांधी आजीवन खूब आलोचनाओं के शिकार हुए। चिट्ठियों में उन्हें लोग जी भरकर गालियाँ देते थे। वे कहते थे गाली और प्रशंसा मेरे लिए एक ही है। मैं इसे समझ सकती हूँ। जब आपका उद्देश्य विराट होता है तब निंदा-प्रशंसा एक ही हो जाती है। बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि उनके किसी कदम पर भक्त या निंदक क्या कह रहे हैं। इसी स्थितप्रज्ञता और महानता के आस-पास कहीं एक तानाशाह मन होता है जिसे बरजते रहना, परखते रहना चाहिए। इस मुद्दे पर आगे बाते करूंगी ही।
सफलता से पहले के गांधी
इस घपले की शुरुआत में मैं उस बोदे आदमी को देखना चाहती हूँ जो अपनी असफलताओं से घबराया हुआ था, सबके सामने बोलने से डरता था, जैसा कि हममे से कोई भी हो सकता था, और है। कमज़ोर और भगौड़े जैसे! अब तक उसके संघर्ष निजी थे।
चोरी करके, माँसाहार करके,सिगरेट पीकर उसने अंतत: पिता को सब चिट्ठी में लिख दिया और रोकर अपनी आत्मा को पवित्र पाया। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार इस अच्छे मारवाड़ी परिवार के लड़के को यह समझ आया कि सामूहिक अस्मिता के सवालों से जूझे बिना वैयक्तिक संघर्षों का इतिहास की नज़र में कोई मोल नहीं है।
आगे के सारे प्रयोगों के बीज यहीं पड़े थे। उसने अपनी कमज़ोरियों पर विजय पाने के लिए एक कठिन और निराली राह चुनी। यह राह थी- ज़िद ! न टूटने वाली ज़िद। सविनय अवज्ञा। पहले दर्जे का टिकट लेकर तीसरे दर्जे में नहीं बैठूंगा भले ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाए।
स्टेशन पर रात गुज़ारनी पड़े।वे पलट के घूसा भी मार सकते थे। अदालत में मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। यह ज़िद गांधी के बहुत काम आई आगे और उनके परिवार की पीड़ा भी बनी।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी
दक्षिण अफ्रीका ने यह तय कर दिया था कि गांधी का जीवन अब सार्वजनिक जीवन ही हो सकता है। वे अकेले में, पत्नी-बच्चों के साथ अपने छोटे से संसार में खुश रह सकने वाले जीव नहीं थे। सार्वजनिक जीवन में उन्हें अपनी उपादेयता महसूस हुई तो यह एक लत बन गई। दक्षिण अफ्रीका में ही अहिंसा और सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण औजार उनके हाथ लग चुके थे जिनके साथ और प्रयोग हिंदुस्तान में अभी किए जाने थे। यहाँ मज़ेदार यह है, और जिस मुख्य बिंदु पर मुझे आना ही है, ये दोनो औजार उन्होने स्त्रियों से प्राप्त किए थे। इसमें संदेह नहीं। अपनी कमज़ोरियों और अक्षमताओं से उलझते हुए उनके लिए कस्तूरबा से निबटना आसान नहीं था। कस्तूरबा की हठ, असहयोग, सहनशीलता और उत्सर्ग उनके लिए एक पथ-प्रदर्शक बने। साथ ही काली औरतों का उनपर गहरा असर हुआ। स्त्रियों के भीतर अहिंसात्मक तरीकों से लड़ने और बात मनवाने, सहते जाने और त्याग करने की अदम्य क्षमता के विविध प्रयोग अभी हिंदुस्तान में किए जाने थे।
मेरी नज़र में इसका सबसे सुन्दर प्रयोग साम्प्रदायिकता के मुद्दों से निपटने में गांधी ने किया। नोआखली में जो हुआ उसे कोई गांधी ही सम्भव कर सकता था। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति जो हिंदुओं से मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए और मुसलमानों से हिंदुओं का पक्ष लेने के लिए आजीवन गाली खाता रहा वह आज फिर से गालियाँ खा रहा है।
औरतों को लेकर क्रांतिकारी नहीं थे गांधी के विचार
यह कोई नई बात नहीं थी।
उन्नीसवीं सदी के समाज-सुधारकों को पढते हुए मैंने यही महसूस किया कि स्त्रियों को लेकर उनकी सोच में कोई नई बात, कोई क्रांतिकारिता नहीं थी। अपनी किताब ‘इण्डियन विमेन’ में गेराल्डाइन फोर्ब्स लिखती हैं कि यूरोप की नज़र में भारत एक अत्यंत पिछ्ड़ा हुआ देश था क्योंकि यहाँ की स्त्रियों की दुर्दशा जैसी दुनिया में कहीं नहीं थी। बाल-विवाह, सती-प्रथा, जहालत, अशिक्षा, अंध-विश्वास, ऊंची मृत्यु-दर, विधवाओं की स्थिति तो अत्यंत शोचनीय थी। ऐसे में सुधारकों को अपने राष्ट्र की छवि सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी लगा कि स्त्रियों को इस नरक से निकाला जाए। लेकिन इन सब सुधारों का अंतिम लक्ष्य एक अच्छी, कुशल, शिक्षित, संस्कारित गृहिणी बनाना ही था। संरचना से टकराने का काम तो औरतों को खुद ही करना था। ज्योतिबा और सावित्री बाई, पंडिता रमाबाई ने यह काम किया भी। लेकिन यह और मज़ेदार है कि बीसवीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन से रमाबाई की आवाज़ गायब कर दी गई। 1922 तक उनके जीवित रहने के बावजूद। महज़ इसलिए कि वे हर स्तर पर संरचना से टकरा रही थीं। संरचना, जो पितृसत्तात्मक ही नहीं थी हिंदू भी थी और रमाबाई दलित से विवाह करके ईसाई हो चुकी थीं।
सबको साथ लेकर चलना गांधी की वह खूबी थी और राष्ट्रीय आंदोलन की विवशता भी कि वे स्त्रियों के लिए कोई क्रांतिकारी ज़मीन तैयार करके अपनी ताकत को कमज़ोर नहीं करा सकते थे। स्त्रियों को अपनी अस्मिता के प्रति सचेत होने देने का मामला बड़ा नाज़ुक मामला था। इससे बड़ा लक्ष्य गांधी के सामने था। मुझे दूधनाथ सिंह की कहानी ‘माई का शोकगीत’ याद आती है। गांधी जी के आंदोलन में जी-जान से लगी माई जब एक दिन अपने गाँव की स्त्री को घर में पिटता देखती हैं तो बापू को चिट्ठी लिखती हैं – देश के गोरे राचछ्सों से आप लड़िए, मेरे लिए गाँव में ही बहुत काम है, यहाँ तो घर-घर में गोरे राच्छस भरे पड़े हैं।
तो गाँधी ने भारत की स्त्रियों के भीतर आत्मोत्सर्ग और सहनशीलता की भावना को चुनौती दी, और बावजूद इसके कि गांधी के भारत आने से पूर्व ही स्त्रियाँ सार्वजनिक जीवन और कामों में आ चुकी थी, उन्होंने स्त्रियों के बाहर निकलने के कारणों को वैधता दी और बड़ी संख्या में उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के हिरावल दस्ते में शामिल कर लिया। वे लिखते हैं –“भारत में स्त्रियों ने पर्दे को फाड़ फेंका और राष्ट्र के लिए काम करने को आगे आई। उन्होंने देखा कि राष्ट्र उनसे महज़ घर की देखभाल के अलावा भी कुछ और चाहता है” इस तरह वे मामूली स्त्रियाँ भी जो सदियों के शोषण और गुलामी की वजह से आत्म-सम्मान खो बैठी थीं उनमें एक गर्व का भाव भरा। देश के लिए उनका होना भी मानी रखता है !
लेकिन स्त्रियों के साथ इस प्रयोग में कई सीमाएँ थीं। विचारों और कर्मों से जो पवित्र हैं वे स्त्रियाँ ही उनके अभियान का हिस्सा हो सकती थीं। स्त्रियों के साथ इस पवित्रता को जोड़ना एक हिंदू सवर्ण की नैतिकता के अलावा क्या था कि 1925 में बंगाल कॉन्ग्रेस द्वारा वेश्याओं को संगठित करने को लेकर वे उखड़ गए ? राधा कुमार अपनी किताब ‘हिस्टरी ऑफ डूइंग’ में इस पर विस्तार से बात करती हैं।
स्त्री होना चाहते थे गांधी
गाँधी स्त्री होना चाहते थे। वे चाहते थे आश्रम के लोग उन्हें बाप नहीं माँ मानें। मनु गाँधी ने उन्हें माँ ही कहा है। एक तरह से यह प्रयोग था।
वे मानते थे कि साधना से पुरुष स्त्रियों के गुण पा सकते हैं। अपने एक सहयोगी कृष्ण्चंद्र को एक पत्र में वे लिखते हैं- ‘the idea is that a man, by becoming passionless, transforms himself into a woman, that is, he includes woman into himself’ स्त्रैण और परुष विशेषताओं का आना-जाना लगे रहना और दुनिया के तमाम लोगों में स्त्रैण-परुष का समान बँटवारा होना एक बराबरी का समाज बनाएगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है।
- यहाँ दो बातें अजीब हैं। हम सब उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के वाकिफ़ हैं। लेकिन पहली बात, ‘पैशनलेसनेस’ से स्त्रीत्व को व्याख्यायित करना दिक्कततलब है।
अपनी किताब ‘द फीमेल यूनक’ में जर्मेन ग्रीयर उसी प्रक्रिया को खोलकर बताती हैं जिसके ज़रिए स्त्री को बधिया बनाया जाता है, आवेगहीन, शमित किया जाता है और फिर मूल्य की तरह यह उसके चरित्र के साथ नत्थी कर दिया जाता है।
- दूसरी बात, दोषहीन, निष्कलंक ब्रह्मचारियों (यानी जो मात्र संतानोतपत्ति के लिए संसर्ग करें) का समाज बनाने का मकसद क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि गाँधी का सारा संघर्ष अपनी कमज़ोरियों के खिलाफ लड़ने से शुरु होता है। यह संघर्ष बड़ा होता जाता है तो समस्त नैसर्गिक मानवीय प्रकृति के खिलाफ एक युद्ध में तब्दील हो जाता है।
भोजन के साथ किए प्रयोग, इलाज के तरीकों में उनके प्रयोग और ब्रह्मचर्य ! सभी में एक सी हठ कि मेरा रास्ता सही है। स्त्री-यौनिकता से यह भय पूरी दुनिया की भिन्न संस्कृतियों का जैसे ज़रूरी हिस्सा है। अकेले में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन आसान है। लेकिन स्त्री के करीब रहकर उसके कामुक प्रभाव से बच निकलना सच्चा संत ही कर सकता है।
सबरीमाला के भगवान तक स्त्री की उपस्थिति से आक्रांत हैं। माया महाठगिनी, पाप का द्वार,नर्क का द्वार। ऐसे में उसे खुद भी पवित्र रहना चाहिए और पुरुष को भी रहने देना चाहिए। संसार की सेवा के लिए अविवाहित स्त्री जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है उससे बेहतर कोई भी नहीं।
ब्रह्मचर्य के प्रयोग अक्षम्य थे
पिता को चिट्ठी लिखकर मोहनदास इतना तो जान गए थे कि जो बात छुपाई जाती है वह पाप है। छिपाने का अपराध-बोध आपको पवित्र नहीं रहने देगा। इसलिए ब्रह्मचर्य के सभी प्रयोगों पर उन्होंने स्वयम बात की। यह साहस श्लाघनीय है। हमारे बीच में से कितने पुरुष स्वीकार कर सकते हैं कि बसों, सार्वजनिक जगहों पर स्त्रियों के बीच वे क्या-क्या महसूस करते रहे? उनके और प्रेमा कण्टक या बाकी के सहयोगियों के बीच का पत्राचार इस साहस का प्रमाण है।
लेकिन जितना गांधी अपने अनुभवों की कहते हैं उन स्त्री-सहयोगियों की भावनाओं की एकदम नहीं बताते जो इन प्रयोगों में साथ थीं। उनका मह्ज़ गिनी पिग बना दिया जाना अक्षम्य है। आश्रम की तमाम स्त्री-सहयोगियों के बीच ईर्ष्या के कई सबूत मिलते हैं। तमाम आलोचनाओं के बाद भी गांधी कहते हैं कि उनकी सहयोगियों की सहमति है तो फिर बाकियों को क्या दिक्कत है?
यहाँ सुचेता कृपलानी के प्रेम विवाह की बात याद करनी चाहिए। गाँधी प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाहों के खिलाफ थे। शायद पूछा भी किसी ने कि जब दो लोग राज़ी हैं तो बाकियों को दिक्कत क्यों? इन तमाम वैचारिक विरोधाभासों पर बात करने से नीलिमा डालमिया तक बच निकलीं हैं जिन्होंने अपनी किताब ‘कस्तूरबा की रहस्यमय डायरी’ में तथ्यों के आधारपर कस्तूरबाई की दृष्टि से एक फिक्शनल किताब लिखी है।
पालना झुलाने वाले हाथों ने आज आज़ादी की मशाल थाम ली लेकिन..
स्त्री को माता बनाया गया और माता को पीड़िता। भारत माता का बिम्ब भी यही था। सरोजिनी नायडू अपने एक भाषण में देश के मर्दों को सम्बोधित करते हुए कहती हैं कि पालना झुलाने वाले हाथों ने आज आज़ादी की मशाल थाम ली है, अब तो शर्म करो भाइयों !
कुल मिलाकर गाँधीवादी आंदोलन में स्त्रियों की हर तरह की हिस्सेदारी ने उन्हें इस तरह भ्रमित किया कि उन्हें अपना असल शत्रु- पितृसत्ता नज़र ही नहीं आई।
वे तो एक पवित्र उद्देश्य में अपने भाइयों, पतियों, पिताओं का साथ देने के लिए पर्दे को फेंककर दुर्गा और काली बन सामने आ गई थीं। सबसे पहला झटका उन्हें तब लगा जब ‘हिंदू कोड बिल’ के समर्थन में वही हिंदू पुरुष खड़े मिले जिनके कंधे से कंधा मिलाकर वे आज़ादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने निकली थीं।
यह भ्रमावस्था लम्बी चलती है। लगभग 1970 तक। यही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप था। आज हम देखते हैं कि उन्नीसवीं सदी के तमाम सुधारकों और राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेताओं गोखले, तिलक, पटेल, जस्टिस रानाडे जैसे तमाम लोगों की धरोहर हिंदू राष्ट्र बनाने के काम आ रही है।
एक बात साफ है कि गहरे अध्ययन के बिना इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी ठसक से कहना निरी मूर्खता है और तमाम अध्ययन के बाद भी इसके बारे में बिना एक पक्ष पकड़े कुछ कहना मुश्किल है।
इतना ज़रूर है कि निजी और सार्वजनिक का भेद जिस तरह यह अपने जीवन में मिटा पाया वह असाधारण है। यह भी कि उसकी क़ीमत आप कभी अकेले नहीं चुकाते। गाँधी ने भी अकेले नहीं चुकाई गाँधी होने की क़ीमत। यह कोलेटरल डैमेज सम्भवतः सबसे ज़्यादा स्त्रियों के पल्ले पड़ा।
असल समस्या अब यह है कि सावरकर और गोडसे जैसों की मौजूदगी की क़ीमत चुकाना एक समाज को इतना भारी और महँगा पड़ता है कि पूरे इतिहास में गाँधी को एक ही बार पाया जा सकता था।
अब, सबको साथ लेकर चलने वाला भी गाँधी नहीं हो सकता, लेकिन गाँधी के रास्ते से गुज़रे बिना यह संभव भी नहीं।
दरअसल, मौलिकता के बिना कोई पीढ़ी अपने युद्ध नहीं जीत सकती। सत्य के साथ उसे अपने प्रयोग करने होंगे।

सुजाता दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। कवि, उपन्यासकार और आलोचक। ‘आलोचना का स्त्री पक्ष’ के लिए देवीशंकर अवस्थी सम्मान। हाल ही में लिखी पंडिता रमाबाई की जीवनी, ‘विकल विद्रोहिणी पंडिता रमाबाई’ खूब चर्चा में है।