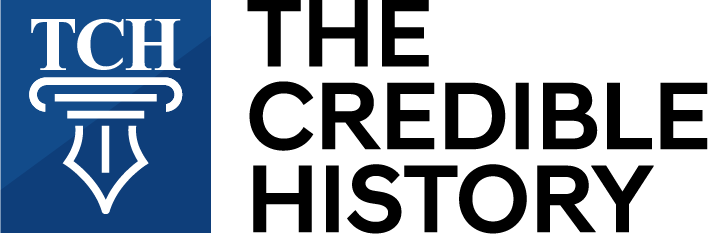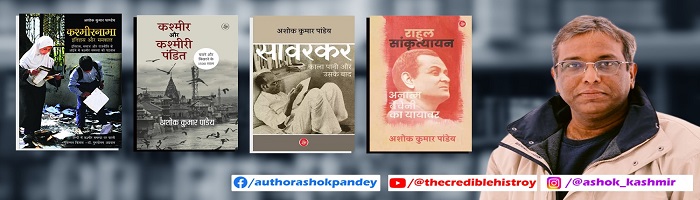शानी, जिनके लेखन में मुस्लिम समाज का यथार्थ मिलता है: जन्मदिन विशेष

साहित्य धारा में कई लेखक ऐसे है जिनकी एक ही कृति ने उनको पाठकों के ज़ेहन में अंकित कर दिया। हर बड़े लेखक के हिस्से में एक ऐसी कृति होती ही है, भले वह उनकी सर्वश्रेष्ठ कृत्ति न हो पर पाठक के जे़हन में लेखक का अगला-पिछला सब गायब हो जाता है और वह एक कृति पाठक के लिए उस लेखक की पहचान बन जाती है।
साहित्यकार गुलशेर खां शानी की काला जल भी एक ऐसी ही रचना है जिसके वो पाठक के दिलो-दिमाग में आज भी ओझल नहीं हुई है। 16 मई, आज गुलेशर खां शानी की जन्मतिथी है। 25 अक्टूबर 1981 को साहित्य अकादेमी सम्मान लेते समय गुलशेर खां शानी दिए गए भाषण का अंश,
क्यों लेखक बनना शानी की नियति थी
… जब आप सबके साथ होते हैं तो अपने साथ नहीं होते और जिस दिन आप अपने साथ हो लेते हैं, बाकी सब कट जाते हैं। इसी अपराध-भार, अकेलेपन, अन्तद्वंद, सन्देह और तलाश में मैंने चुपचाप कलम उठा ली थी और किसी को कानों-कान पता नहीं था।
मैं लेखक बन गया था। क्योंकि यही मेरी नियति थी। मैं और कुछ हो भी नहीं सकता था। आन्तरिक तनावों, दवाबों, हीन भावनाओं और अनेक ग्रन्थियों का शिकार मैं शायद ऐसे ही एक मंडवे की तलाश में था जिसमें मैं अपने को छिपा सकूं। लेखने मेरे लिए वैसा ही शरणस्थल था। मेरे सामने न तो कोई सामाजिक उद्देशय था और न किसी प्रकार की प्रतिबद्धता।
मैं तात्कालीन किसी सामाजिक या राजनीतिक आन्दोलनों से भी परिचित नहीं था। और न किसी सामाजिक अन्याय ने मुझे लेखन की ओर प्रेरित किया था। लिखना मेरे लिए नितान्त व्यक्तिगत, निजी और गोपन यन्त्राणाओं से मुक्ति और कुछ तंग करने वाले प्रश्नों से जूझने का माध्यम था और आज भी है।
मेरी रचनाएं इलाहाबाद और बनारस की कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। कुछ प्रशंसाएं मिली थीं। पत्र आने लगे थे और मुझे हलके से अपनी विशिष्टता का एहसास होने लगा था। यह अच्छा और बुरा दोनों था, क्योंकि जहां इसने रहे-सहे एकाध दोस्तों से काटकर सारे कस्बे में मुझे अकेला कर दिया था, वहीं मुझे यह अवसर भी दिया कि मैं अपनी छोटी-सी दुनिया गढ़कर उसमें डूब जाऊं। वह दुनिया थी मेरा छोटा-सा कमरा, जिसमें अक्सर सिर्फ धनंजय वर्मा आया करता था।
किस जगह की कोई सांस्कृतिक परम्परा न हो, जहां साहित्यकार तो साहित्यकार, ढंग का साहित्य भी न आता हो, जहां टुटरू-टूं ही रियासती लाइब्रेरी हो और उसमें भी बाबा आदम के जमाने की अनपढ़ी किताबें भरी हों, वहां आदमी लेखक भले बन जाए, साहित्यकार होने का सपना कितना दुखदायी हो सकता है, इसे कम लोग समझ पाएंगे।
खासकर मेरे जैसे आदमी के लिए जो हाई स्कूल के बाद एक सहकारी संस्था में किरानीगिरी या क्लर्की कर रहा था और जिसने कभी भी कांलेज या विश्वविद्यालय का अहाता भी नहीं देखा था। मुझे उन सब दोस्तों से ईष्या थी जो मुझे कस्बे में छोड़कर ऊंची शिक्षा के लिए बाहर के बड़े शहरों को चले गए थे और आगे बढ़ते चले जा रहे थे, धनंजय वर्मा भी उनमें से एक था।
तब मुझे एहसास भी नहीं था कि अनजाने ही मैं एक दौड़ में शामिल हो गया हूं। एक ऐसी साहित्यक दौड़ में, जिसमें इलाहाबाद, बनारस, आगरा और दिल्ली जैसे शहरों के मुझसे दस गुना सक्षम, समर्थ और साधन-सम्पन्न लोग भाग ले रहे हैं। मेरी स्थिति एक ऐसे प्रतियोगी की तरह थी जो दौड़ने के लिए तैयार साथियों की अपेक्षा दस फुट नीचे गडढ़े में खड़ा था। लिहाजा मेरी आधी शक्ति ऊपर आने की कोशिश में ही जाया हो रही थी। इलाहाबाद की यात्रा एक ऐसी ही कोशिश थी।
प्रेमचंद से उपेन्द्र नाथ अश्क तक की साहित्यक संगत
स्कूल के ज़माने में ही प्रेमचंद, यशपाल, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र और अज्ञेय वगैरह को पढ़ रखा था। कुछ बाद में मैंने उपेन्द्र नाथ अश्क के उपन्यास पढ़े। आज भी मुझे हैरानी होती कि अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें और गर्म राख पढ़कर मैं कैसे अभिभूत हो गया था। अपनी कच्ची ज़हनियत और अपरिपक्वता के कारण अज्ञेय या यशपाल या तो मेरी समझ के बाहर थे या फिर शायद अश्क के सतही विवरणात्मकता वाले कलाहीन और स्किन डीप उपन्यास मेरी तात्कालीन मानसिकता और सूझ-बूझ के निकट पड़ते थे।
जो हो, अश्क जी से पत्राचार, मेरी इलाहाबाद यात्रा, अश्कजी से भेंट, उनकी बहुचर्चित जिश्न्दादिली और इलाहाबाद में कुछ बड़े लेखकों के साथ गुजारे दिनों का अनुभव, यह सब लम्बी चर्चा का विषय है और यहां अप्रासंतिक भी। लौटो तो मेरी नाखूनों से भरी हुई मिट्टी काफी उतर चुकी थी।
उन दिनों भैरव प्रसाद गुप्त के सम्पादन में निकलने वाली कहानी की बड़ी धूम थी। कई दृष्टियों से यह पत्रिका ऐसी थी कि उसमें सारे साहित्य-जगत का ध्यान खींच रखा था। कहानी के कई ऐतिहासिक विशेषांक निकले थे और सौभाग्यवश मेरी पहली कहानी के ऐसे ही विशेषांक में छपी थी।
तब कहानी में एक बार भी छपना हिन्दी-जगत में परिचय के लिए काफी था। मैं गुमनामी के जिन्दगी से धीरे-धीरे बाहर आ रहा था। तभी नीलाभ प्रकाशन से मेरा पहला कहानी-संग्रह बबूल की छांव छपकर आया और मैं सहसा साहिबे-किताब बन गया।
आज सोचता हूं तो लगता है कि जिस अश्क-संसर्ग को मैं अपनी जिन्दगी की सुखद और सौभाग्यपूर्ण घटना समझ रहा था, वह मेरी साहित्यक जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस भूल का खामियाजा मुझे बहुत दिनों तक अदा करना पड़ा।
अश्क की तकलीफ यह है कि दुनिया इनके इर्द-गिर्द क्यों नहीं घूमती और मेरी तकलीफ यह है कि अपने लेखकीय संघर्ष का बहुत मासूम और आरम्भिक समय मैंने अश्क से सम्बद्ध होता है, ग्यालियर की याद बदकिस्मती से मेरे लिए ऐसी ही है।
क्या सबक सिखाया, ग्वालियर शहर ने शानी को…
यों मैने जगदलपुर से ग्लालियर जाने का स्वागत किया था। उस सुदूरवर्ती कोने में पड़े हुए और सब-कुछ से कटे-छंटे कस्बे से मुक्ति, जैसे अपने भौगोलिक, मानसिक और अनुभव-संवेदना के सीमित क्षितिज से बाहर आना था। बावजूद जिम्मेदारियों के नए बोझ के, मुझे यह अच्छा लगा और मैं खुश था। अभी थोड़े ही दिन हुए थे।
अभी मैं ऐतिहासिक नगरी में सहसा पहुंचने के सम्मोहन में बंधा हुआ था। आसमानी पहाड़ियों, पारदर्शी जल और ताहद्देनजर सब्जा-जार देखने की आदी आंखो में अभी कांटेदार छोटी-छोटी झाड़ियों, ऊंट जैसी बदशक्त और बदरंग मिट्टी के दूहों और मुहकमा जंगलात के मैल और फटे हुए तम्बू जैसे आकाश से समझौता भी नहीं किया था कि दो छोटी-छोटी घटनाएं हो गई थीं।
वह एक सरकारी पत्र के सह-सम्पादकों का कक्ष था और मेरी तीसरी नौकरी थी। मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक रिहायशी मकान की तलाश में था और दफ्तर के कई साथियों ने मेरी सहायता के झूठे सच्चे वादे कर रखे थे। मित्रों को मैं रोज कोंचा करता था। उन्हें भी याद दिलाया। वह उसी रियासिती सरदार परिवार से सम्बद्ध, ग्वालियर के खानदानी बाशिन्दे और महाराष्ट्रियन सज्जन थे।
मिल जाएगा, वह तसल्ली देते हुए बोले, जल्दी ही दिला दूंगा।
शुक्रिया, मैंने कहा था, लेकिन सुनिए, एक बात याद रखोंगे? मकान जहां तक हो सके, मुस्लिम मोहल्ले में न हो तो बेहतर होगा।
सरकारी दफ्तरों में इनीशियल्स चलते हैं। मेरे भी थे। लेकिन मैं शानी के नाम से ही जाना जाता था। मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि वह मेरे पूरे नाम से परिचित नहीं हैं। मुस्लिम मोहल्ले में मकान न लेने की बात मैंने इसलिए कही थी कि मैं घोर धार्मिक वातावरण और कट्टरपन्थी माहौल से दूर रहना चाहता था।
क्यों? उन्होंने चौकते हुए पूछा, मान लें, अगर वैसे ही मोहल्ले में मकान मिल गया तो क्या बुराई है?
कहकर एकाध पल वह मुझे घूरते रहे। फिर मेरे कान के पास झुकते हुए और मुझे पूरी तरह कान्फिडेन्स में लेकर वह धीरे-से बोले, सुनिए, डरने की कोई बात नहीं। आप बिल्कुल मत डरिए। यहां साले मियां लोगों को इतना मारा है इतना मारा है कि अब आंख उठाने की हिम्मत नहीं रही।
चाहे इसकी और इस जैसी दो-तीन घटनाओं की प्रतिक्रिया थी या संयोग, मकान आखिर मुझे मिला भी तो एक घोर मुस्लिम मोहल्ले में और मैंने कोई आपत्ति नहीं की। वह एक बाड़ा था, जिसमें चार-छह मकानात थे और हमारी दहलीज से मस्जिद का जीना शुरू होता था।
नए घर में तीसरी या चौथी सुबह जब बाहर का दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि हमारी चौखट के पास गाय का गोश्त और कुछ हड्डियां फैलाई गई हैं। यह सिर्फ शरारत नहीं थी, मोहल्ले के कुछ उत्साही लड़कों के द्वारा विरोध और गुस्से का प्रदर्शन था ताकि मैं मकान छोड़कर भाग जाऊं।
विरोध इस बात का कि मकान-मालिक ने मोहल्लेदारी की परम्परा और उसूल के खिलाफ साहनी साहब नाम के किसी पंजाबी को मकान क्यों दे रखा है। खासकर इसलिए कि बाड़े की मस्जिद का जीना उसी काफिर की दहलीज से होकर जाता था और वह खानए-खुदा की तौहीन थी।
खुदा और सनम, दोनों को मैं पीछे छोड़ आया था। घोर नास्तिक न सही, मैं सौ-फीसदी सन्देहवादी बन गया था और जाहिर है कि सन्देह या तर्क का इस्लाम में कभी कोई मौका नहीं होता। मेरा घर धर्म या संस्कार नहीं, संस्कृतिगत अर्थों में मुस्लिम था और वह आज भी है।
मैने ऐसे महौल में होश सम्भाला था जहां धर्म, नैतिकता की तरह, व्यक्ति और समाज, दोनों का बिल्कुल जाती मामला था और भाग्यवश साम्प्रदायिकता की बू तक नहीं पहुंची थी। शायद इसीलिए कि एक अरसे तक मैंने इस पर सोचा भी नहीं था।
फिर जब सोचा तो हैरानी है कि अपने को हमेशा अलग करके क्यों सोचा? ऐसे मानों, मैं इसकी जद में न तो आता हूं और न कभी आऊंगा। मुझे ग्वालियर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे यह भी सबक की तरह समझाया।
मैं वहीं खड़ा हूँ, जहाँ से चला था
मेरी पहली कहानी सन 1957 के आसपास छपी थी। अब बाईस साल हो गए। इस बीच बहुत सा पानी सिर पर से गुजर गया लेकिन मैं वहीं खड़ा हूं जहां से चला था। कोई साठ-पैंसठ कहानियां लिखी होंगी ज्यादा-से-ज्यादा सत्तर। उनमें से चुनी हुई और मेरी महत्वपूर्ण कहानियों की यह पहली जिल्द है, सब एक जगह।
कहानियों की अन्तर्विरोधों, तकलीफों, आन्तरिक यातना और विसंगतियों की कहानियं हैं। लगभग बीस बरस पहले इसी वर्ग की मेरी कहानी जली हुई रस्सी से लेकर नवीनतम कहानी बिरादरी तक की यात्रा का जायज़ा लेते हुए मुझे लगता है जैसे मौटे तौर पर मेरी रचना के तीन पड़ाव हैं, अपनी तरह के तीन शिफ्ट लिए हुए।
हालांकि साथ में यह भी लगता है कि भावभूमि की दृष्टि से आज मैं जहां खड़ा हूं वह तो मूलत: वही है जिसकी यात्रा मैंने जली हुई रस्सी से अनजाने ही आरम्भ कर दी थी।
आज मैं ज्यादा गहरे विश्वास के साथ काम कर रहा हूं और करते रहना चाहता हूं कि सच्ची रचनाकारिता के लिए कथानक ज्यादातर अपने आसपास और अपनी ही वर्ग में देखे जाने चाहिए।
वैसे भी इस बात की जरूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा है कि ऊपर-ऊपर से लिए हुए भोले विश्वास पर सन्हेह करने वाली यह छानबीन जातीय संवेदनाओं और वर्णगत संस्कारों तक गहराई से की जाए। व्यक्तिगय रूप से जहां तक मैं समझता हूं अपने सारे आधुनिकीकरण के बावजूद हमने बहुत-कुछ ऐसा बचा रह जाता है जो घर, समाज, धर्म और इतिहास हमें विरासत से सौंपकर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं और जिनकी जड़ों की गहराई का कई बार हमें पता नहीं होता।
ताज्जुब है कि उनके तात्कालिक सन्दर्भ जहां हमें चेतन रूप में परेशान कर रहे होते हैं वहीं दूसरी ओर अजनाने से वे ही परिचालित भी करते हैं। यह एक अजीब, मारक लेकिन फितरी जद्दोजहद होती है। आप उसी से लड़ते हैं जो आपकी शक्ति होती है क्योंकि यही और यही विडम्बना शायद मानवीय नियति है।
(विशेष, आभार shaanifoundation.org जहां से यह अंश लिया गया है।)
जनता का इतिहास, जनता की भाषा में